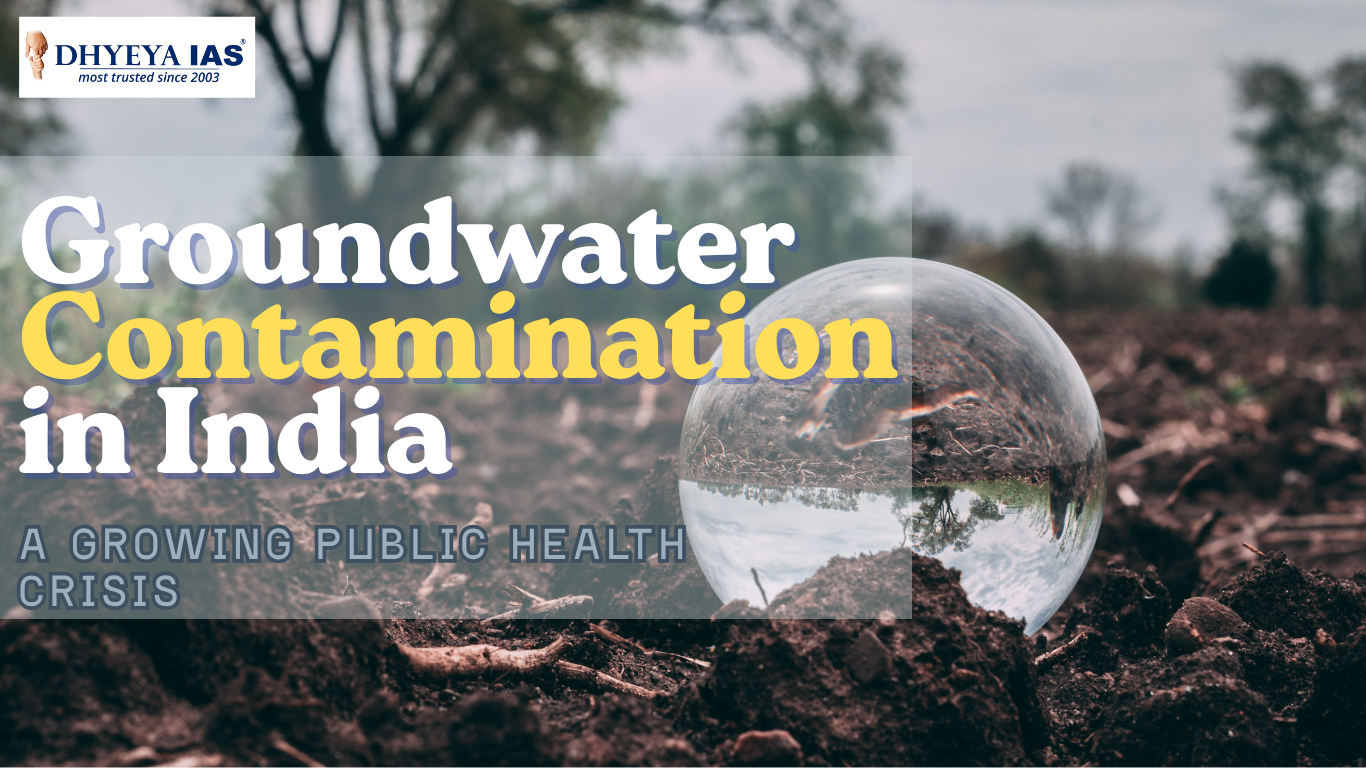भारत को अक्सर नदियों और मानसून की धरती के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन इस छवि के पीछे एक सच्चाई छिपी है—देश की अधिकांश बुनियादी जरूरतें सतही जल नहीं बल्कि भूजल पूरा करता है। यह ग्रामीण पेयजल का 85% से अधिक और सिंचाई जल का लगभग 65% प्रदान करता है, जिससे यह घरेलू और कृषि दोनों के लिए जीवनरेखा बन जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, अत्यधिक और अक्सर अनियमित दोहन ने न केवल जलभृतों को खत्म कर दिया है बल्कि और अधिक खतरनाक खतरा पैदा कर दिया है व्यापक भूजल प्रदूषण के रूप में।
एक समय प्रकृति के सबसे शुद्ध भंडारों में गिना जाने वाला भूजल अब कई क्षेत्रों में नाइट्रेट, भारी धातु, औद्योगिक रसायन, रेडियोधर्मी तत्व और रोगजनक जीवाणुओं से दूषित हो चुका है। यह प्रदूषण अक्सर अदृश्य होता है, धीरे-धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में समा जाता है, लेकिन यह लाखों लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।
समस्या की गंभीरता
केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) की 2024 की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। देश के 440 जिलों से नमूने लेकर किए गए परीक्षण में पाया गया:
· 20% से अधिक नमूनों में नाइट्रेट प्रदूषण, जो मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और खराब सेप्टिक सिस्टम से रिसाव के कारण है।
· 9% से अधिक नमूनों में सुरक्षित सीमा से ऊपर फ्लोराइड स्तर, जिससे राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव देखे गए।
· पंजाब और बिहार के कुछ हिस्सों में डब्ल्यूएचओ की 10 µg/L सीमा से अधिक आर्सेनिक प्रदूषण, जो कैंसर और तंत्रिका संबंधी विकारों से जुड़ा है।
· पंजाब, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में 100 ppb से अधिक यूरेनियम की सांद्रता—जिसका कारण फॉस्फेट उर्वरक का उपयोग और अत्यधिक भूजल दोहन है।
· 13% से अधिक परीक्षण किए गए नमूनों में लोहे का प्रदूषण, जो जठरांत्र और विकास संबंधी समस्याओं में योगदान देता है।
ये केवल आंकड़े नहीं हैं—ये लंबे समय से उपेक्षा, कमजोर नीतिगत प्रवर्तन और ठोस रोकथाम कार्रवाई की अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
भारत में भूजल मृत्यु क्षेत्र
कुछ स्थानों पर, प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि इससे तात्कालिक और स्पष्ट त्रासदियां सामने आई हैं:
· बुधपुर, बागपत (उ.प्र.) में, दो सप्ताह के भीतर 13 लोगों की मौत किडनी फेलियर और संबंधित जटिलताओं से हुई—संभावना है कि यह पास की पेपर और शुगर मिलों से जहरीले औद्योगिक अपशिष्ट के कारण बोरवेल जल के प्रदूषण से जुड़ा है।
· जालौन (उ.प्र.) में, निवासियों ने हैंडपंप से पेट्रोलियम जैसी गंध वाले तरल निकलने की शिकायत की, जो संभवतः भूमिगत ईंधन रिसाव के कारण था।
· पैकारापुर, भुवनेश्वर में, एक खराब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ने गंदे पानी को भूजल में रिसने दिया, जिससे सैकड़ों लोगों में सामूहिक बीमारी फैल गई।
ऐसी घटनाएं अलग-थलग नहीं हैं। ये कमजोर प्रवर्तन, अपर्याप्त निगरानी और मूलतः भूमिगत इस आपदा के प्रति सार्वजनिक जागरूकता की कमी के एक सतत पैटर्न को दर्शाती हैं।
स्वास्थ्य पर प्रभाव
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और डब्ल्यूएचओ इंडिया के अध्ययनों से पुष्टि होती है कि दूषित भूजल एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है।
फ्लोराइड
· 20 राज्यों के 230 जिलों में मौजूद, फ्लोराइड प्रदूषण लगभग 6.6 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है।
· स्केलेटल फ्लोरोसिस, एक दर्दनाक और अपंग करने वाली बीमारी है, जो जोड़ों में जकड़न, हड्डियों में विकृति और बच्चों में अवरुद्ध विकास का कारण बनती है।
· राजस्थान में 11,000 से अधिक गांव प्रभावित हैं।
· झाबुआ (म.प्र.) में फ्लोराइड 5 mg/L से अधिक है, और 40% आदिवासी बच्चे प्रभावित हैं।
· उन्नाव (उ.प्र.) में, 3,000 से अधिक हड्डी विकृति के मामले दर्ज हुए हैं।
· 2024 की CGWB रिपोर्ट में 15,259 नमूनों में से 9.04% नमूने डब्ल्यूएचओ की 1.5 mg/L सीमा से ऊपर पाए गए, जिसमें सोनभद्र (उ.प्र.) में 52.3% की प्रचलन दर और शिवपुरी (म.प्र.) में 2.92 mg/L स्तर पाया गया।
आर्सेनिक
· गंगीय क्षेत्र में केंद्रित—पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम सहित।
· लंबे समय तक संपर्क से त्वचा पर घाव, गैंग्रीन, श्वसन रोग, और त्वचा, गुर्दा, यकृत, मूत्राशय और फेफड़ों के कैंसर होते हैं।
· 2021 में नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन ने पाया कि उच्च रक्त आर्सेनिक स्तर वाले प्रत्येक 100 में से 1 व्यक्ति को कैंसर का उच्च खतरा था।
· बलिया (उ.प्र.) में आर्सेनिक 200 µg/L तक पहुंच गया—डब्ल्यूएचओ सीमा से 20 गुना अधिक—जो 10,000 से अधिक कैंसर और बीमारी के मामलों से जुड़ा है।
· भोजपुर और बक्सर (बिहार) में भी इसी तरह के रुझान देखे गए।
· 2024 की CGWB रिपोर्ट ने उ.प्र. के 29 जिलों में असुरक्षित आर्सेनिक स्तर दर्ज किए, जिसमें बागपत में 40 mg/L की भयावह मात्रा पाई गई—जो सुरक्षित सीमा से 4,000 गुना अधिक है।
नाइट्रेट
· विशेष रूप से उत्तरी भारत में आम, नाइट्रेट शिशुओं के लिए खतरनाक है।
· जब नाइट्रेट युक्त पानी से शिशु आहार तैयार किया जाता है, तो यह मेटहेमोग्लोबिनेमिया या “ब्लू बेबी सिंड्रोम” का कारण बन सकता है।
· 2023 के नेशनल हेल्थ प्रोफाइल ने पांच वर्षों में नाइट्रेट विषाक्तता के कारण अस्पताल में भर्ती मामलों में 28% वृद्धि दर्ज की, खासकर पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक में।
· अब भारत के 56% जिलों में नाइट्रेट सुरक्षित सीमा से अधिक है।
यूरेनियम
· पहले केवल चुनिंदा भूगर्भीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला यूरेनियम अब भूजल के अत्यधिक दोहन और उर्वरक उपयोग के कारण अधिक आम हो गया है।
· पंजाब के मालवा क्षेत्र में, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में यूरेनियम स्तर डब्ल्यूएचओ की 30 µg/L सीमा से अधिक पाए गए।
· 66% नमूनों ने बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा किया, और 44% वयस्कों के लिए भी खतरनाक थे।
भारी धातुएं
· सीसा, कैडमियम, क्रोमियम, पारा औद्योगिक अपशिष्ट से जलभृतों में प्रवेश करते हैं।
· ये धातुएं मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकती हैं, एनीमिया पैदा कर सकती हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकती हैं, और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
· ICMR–NIREH अध्ययनों में कानपुर (उ.प्र.) और वापी (गुजरात) के बच्चों में खतरनाक रूप से उच्च रक्त सीसा स्तर पाए गए।
सूक्ष्मजीव प्रदूषण
· रिसते हुए सेप्टिक टैंक और सीवेज के घुसपैठ से हैजा, पेचिश, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E के बार-बार प्रकोप होते हैं।
· पैकारापुर, भुवनेश्वर में, हाल ही में सीवेज-प्रदूषित भूजल से 500 से अधिक लोग बीमार पड़ गए।
संरचनात्मक कारण
संकट की जड़ें नियामक खामियों, कमजोर प्रवर्तन और खराब डेटा पारदर्शिता में हैं:
· जल अधिनियम (1974) भूजल प्रदूषण को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता।
· CGWB के पास वैधानिक प्रवर्तन शक्तियां नहीं हैं।
· राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पुरानी स्टाफ कमी और संसाधनों की कमी है।
· प्रदूषकों के लिए दंड न्यूनतम हैं और शायद ही कभी लागू किए जाते हैं।
· प्रदूषण डेटा तक सार्वजनिक पहुंच सीमित है।
· भूजल का अत्यधिक दोहन आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे प्राकृतिक रूप से मौजूद विषाक्त पदार्थों को सक्रिय कर देता है।
नीतिगत खामियां
वर्तमान में, भारत के पास कोई राष्ट्रीय भूजल प्रदूषण नियंत्रण ढांचा नहीं है। जिम्मेदारियां पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक विनियमन संभालने वाली एजेंसियों में बंटी हुई हैं, और सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी तथा जल गुणवत्ता निगरानी प्रणालियों के बीच समन्वय कमजोर है।
आगे की राह
नियम, तकनीक और सामुदायिक भागीदारी को मिलाकर बहु-आयामी दृष्टिकोण आवश्यक है:
नियामक सुधार
· CGWB को वैधानिक प्रवर्तन शक्तियां प्रदान करना।
· राज्य और जिला स्तर पर स्पष्ट जवाबदेही स्थापित करना।
निगरानी और डेटा एकीकरण
· वास्तविक समय सेंसर और उपग्रह जलभृत मानचित्रण का उपयोग करना।
· जल गुणवत्ता डेटा को HMIS जैसे स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियों से जोड़ना।
तात्कालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप
· पहचाने गए हॉटस्पॉट में आर्सेनिक और फ्लोराइड हटाने की इकाइयां लगाना।
· सुरक्षित पाइप पेयजल तक पहुंच का विस्तार करना।
औद्योगिक और कृषि उपाय
· उद्योगों में ज़ीरो-लिक्विड-डिस्चार्ज सिस्टम अनिवार्य करना।
· अपशिष्ट जल और लैंडफिल रिसाव की कड़ी निगरानी करना।
· जैविक या कम-रसायन आधारित खेती को बढ़ावा दें और किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन पर प्रशिक्षण देना।
सामुदायिक भागीदारी
· पंचायतों, स्कूलों और स्थानीय समूहों को जल परीक्षण में शामिल करना।
· सामुदायिक निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली को प्रोत्साहित करना।
निष्कर्ष
भारत की भूजल चुनौती अब केवल कमी का सवाल नहीं, बल्कि सुरक्षा का भी है। 60 करोड़ से अधिक लोग इस पर निर्भर हैं और प्रदूषण एक पूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में उभरा है। जब तक इसे तात्कालिक कानूनी सुधारों, संस्थागत मजबूती और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के जरिए संबोधित नहीं किया जाता, तब तक मानव स्वास्थ्य और जल सुरक्षा को हुआ नुकसान अपरिवर्तनीय हो सकता है।
|
मुख्य प्रश्न: भारत में भूजल प्रदूषण एक मौन किन्तु व्यापक खतरा है। इससे क्या नैतिक और प्रशासनिक दुविधा उत्पन्न होती है और इसका समाधान कैसे किया जाना चाहिए? |