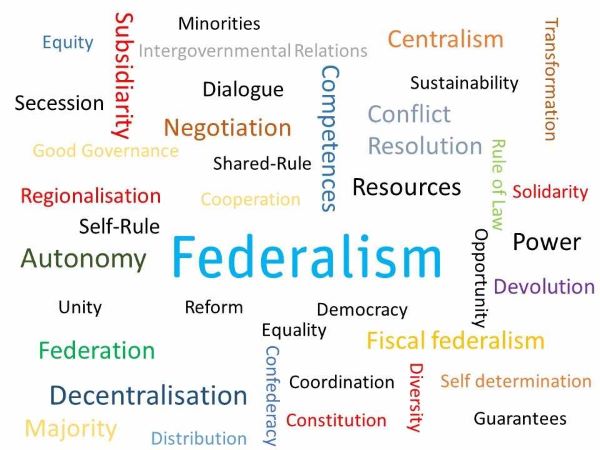तारीख Date : 22/11/2023
Relevance: जीएस पेपर 2 - राजव्यवस्था - राज्यपाल की भूमिका
Keywords: अनुच्छेद 200, विवेकाधीन शक्तियाँ,संवैधानिक ढांचा, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग
Context-
भारतीय राज्यों में राज्यपालों की स्थिति एक बार फिर जांच के दायरे में आ गई है, जिसका उदाहरण तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल में घटित हाल की घटनाएं हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त किया गया हालिया असंतोष राज्यों द्वारा सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयकों पर राज्यपालों की कार्रवाई में देरी पर चिंताओं को उजागर करता है।
विधेयकों के संबंध में राज्यपालों में निहित शक्तियां:
अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के विकल्प:
अनुच्छेद 200 राज्यपालों को राज्य विधानमंडल से विधेयक प्राप्त करने पर चार विकल्प प्रदान करता है:
- विधेयक पर सहमति देना।
- सहमति रोक देना, जिससे विधेयक अस्वीकृत हो सकता है।
- विधेयक (गैर-धन विधेयक) को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाना।
- विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखना।
विवेकाधीन शक्तियाँ:
उच्चतम न्यायालय ने, जैसा कि शमशेर सिंह (1974) जैसे मामलों में निर्णय लिया गया था; इस बात पर जोर देता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी देते समय या वापस करते समय विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। उनके कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं, जैसा कि अनुच्छेद 163 में कहा गया है, (विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त)।
सहमति रोकने का परिदृश्य:
निजी सदस्यों के विधेयकों के लिए या ऐसे मामलों में जहां मौजूदा सरकार ऐसी कार्रवाई चाहती है, सहमति रोकने की दुर्लभ स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि, बहुमत रखने वाली मंत्रिपरिषद आम तौर पर अवांछनीय विधेयकों को पारित होने से रोकती है।
राज्यपाल का विवेक:
राज्यपालों को उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाले या केंद्रीय कानूनों के साथ टकराव वाले विधेयकों को आरक्षित रखना चाहिए। जब उन्हें लगता है कि कोई विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है तो वे अपने विवेक का प्रयोग कर इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। विशेष रूप से, राज्यपालों के लिए निर्णय लेने के लिए कोई संवैधानिक समय सीमा नहीं है।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
औपनिवेशिक विरासत
- भारत में गवर्नर शिप की औपनिवेशिक विरासत लंबे समय से विवाद का मुद्दा रही है। मूल रूप से प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करने का इरादा था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों से राज्य स्तर पर राष्ट्रपति के समकक्ष के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की गई थी।
- हालाँकि, व्यावहारिक वास्तविकता ने उन्हें केंद्र सरकार के एजेंटों के रूप में अधिक कार्य करते देखा है, जो अक्सर लोकप्रिय रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं।
संवैधानिक ढांचा
- राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर उनकी नियुक्ति और निष्कासन प्रक्रियाओं में निहित है। राष्ट्रपति के विपरीत, जिसे देश के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- इसके अलावा, जबकि राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, राज्यपालों को केंद्र सरकार की इच्छा पर हटाया जा सकता है। यह विषमता राज्यपाल की जवाबदेही और उनकी शक्तियों के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता पैदा करती है।
संविधान सभा के दौरान भविष्यवाणियाँ और आलोचनाएँ
- संविधान सभा की बहस के दौरान, औपनिवेशिक प्रभाव और सत्ता के केंद्रीकरण के बारे में प्रश्न उठाये गए।
- दक्षिणायनी वेलायुधन और अन्य सदस्यों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रशासन की विरासत से अलग होने की आवश्यकता पर बल देते हुए 1935 के अधिनियम के प्रावधानों की नकल करने के लिए संविधान के मसौदे की आलोचना की।
अम्बेडकर का औचित्य
- बी.आर. अम्बेडकर ने राज्यपालों से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को बनाए रखने को उचित ठहराते हुए तर्क दिया कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में बदलाव करने के लिए सीमित समय था।
- उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यपाल राज्य सरकारों के साथ काम करने के लिए होते हैं। हालांकि, उन्होंने उस संभावित परिदृश्य को संबोधित नहीं किया जहां राज्यपाल राज्य की तुलना में केंद्र के हितों के साथ अधिक तालमेल बिठा सकते हैं।
मुद्दे और चुनौतियाँ:
- कुछ मामलों में, राज्यपालों ने मंत्रिस्तरीय सलाह के विरुद्ध विधेयकों को लौटाने में विवेक का प्रयोग किया है, जिससे कभी कभी कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय "जितनी जल्दी हो सके" वाक्यांश का उपयोग करते हुए त्वरित निर्णय लेने की संवैधानिक अपेक्षा पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त, असहमति के दौरान सार्वजनिक सहभागिता के लिए कोई निर्दिष्ट प्रक्रियाएँ नहीं हैं।
विभिन्न समिति की सिफारिशें:
- सरकारिया आयोग (1987): इस आयोग का सुझाव है, कि दुर्लभ मामलों को छोड़कर, राज्यपालों की विवेकाधीन शक्ति सीमित है। यह राष्ट्रपति को विधेयकों के निपटान के लिए अधिकतम छः महीने की अवधि की सिफारिश करता है।
- पुंछी आयोग (2010): राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए छह महीने की समय-सीमा का प्रस्ताव करता है, लेकिन ये सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं।
आगे का रास्ता:
- राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने में देरी के उभरते परिदृश्य को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय से एक उचित समय सीमा स्थापित करने का आग्रह किया गया है। यह दृष्टिकोण निर्माताओं के इरादे के अनुरूप है और संवैधानिक ढांचे के भीतर संघवाद के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करता है।
निष्कर्ष
निष्कर्षतः, भारत के संघीय लोकतंत्र में राज्यपालों की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन और सुधार करने का समय आ गया है। औपनिवेशिक संस्था, हालांकि मूल रूप से राज्य सरकारों पर नियंत्रण के रूप में कार्य करने का इरादा रखती थी, अक्सर इसकी सीमाओं को पार करने और केंद्र सरकार के हितों की सेवा करने के लिए आलोचना की गई है।
यह पूर्ण उन्मूलन की वकालत करने के बजाय, अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण में न्यायिक हस्तक्षेप और संवैधानिक सुधार शामिल है। राज्यपालों को राज्य विधानमंडल के प्रति जवाबदेह बनाकर, भारत अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत कर सकता है और एक अधिक संतुलित संघीय ढांचा सुनिश्चित कर सकता है। यह एक जीवंत लोकतंत्र की उभरती जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ राज्यपाल कार्यालय को संरेखित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-
- अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत की संघीय प्रणाली में उनकी विवेकाधीन शक्तियों का आकलन करें। विधेयकों पर राज्यपालों के कार्यों पर चिंताओं को उजागर करने वाली हाल की घटनाओं का विश्लेषण करें और सरकारिया और पुंछी आयोग जैसी समितियों की सिफारिशों का मूल्यांकन करें। (10 अंक, 150 शब्द)
- भारतीय राज्यपालों की ऐतिहासिक विरासत की जांच करें, उनके औपनिवेशिक मूल और संविधान सभा की बहस के दौरान उठाई गई चिंताओं का पता लगाएं। सुधारों का प्रस्ताव रखें और भारत के संघीय लोकतंत्र में अधिक जवाबदेह और संतुलित शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करें। (15 अंक, 250 शब्द)
Source- Indian Express