संदर्भ:
हाल ही में भारत सरकार ने 25 जुलाई 2025 को पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए। इन नियमों का उद्देश्य देशभर में दूषित स्थलों की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और वैज्ञानिक ढंग से उपचार सुनिश्चित करना है। साथ ही, इनका लक्ष्य प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व तय करना और जनभागीदारी को सशक्त बनाना भी है, ताकि पर्यावरणीय न्याय और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके।
2025 नियमों की मुख्य विशेषताएँ:
1. स्थल की पहचान के लिए संरचित प्रणाली
· राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) और स्थानीय निकायों को यह अधिकार दिया गया है कि वे संदेहास्पद स्थलों की पहचान कर सकें, जिनके आधार हो सकते हैं:
- औद्योगिक गतिविधियाँ
- पुराने समय में कचरे का अनियमित निपटान
- स्थानीय लोगों की शिकायतें
2. केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा एक पोर्टल संचालित किया जाएगा, जिसमें सभी दूषित स्थलों की जानकारी दर्ज होगी।
• यह पारदर्शिता बनाए रखेगा, डेटा को ट्रैक करने और राज्यों के बीच समन्वय में मदद करेगा।
3. जोखिम आधारित वैज्ञानिक मूल्यांकन
• पहले प्रारंभिक जांच होगी, फिर विस्तृत स्थल परीक्षण किए जाएँगे।
• यदि किसी स्थल में जोखिम की निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण पाया जाता है, तो उसे “दूषित स्थल” घोषित किया जाएगा और उसकी सफाई अनिवार्य होगी।
4. प्रदूषक भुगतान सिद्धांत लागू
• 90 दिनों के भीतर उस व्यक्ति/कंपनी की पहचान करनी होगी जो प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार है।
• ऐसे ज़िम्मेदार लोगों को पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी।
• जब तक स्थल की सफाई पूरी तरह प्रमाणित नहीं हो जाती, तब तक वहाँ ज़मीन की बिक्री या उपयोग में बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
5. जब प्रदूषण करने वाला ज्ञात न हो, तब सरकार का हस्तक्षेप
• यदि प्रदूषण करने वाला नहीं मिला, तो सफाई का खर्च इन स्रोतों से उठाया जा सकता है:
o “पर्यावरण राहत कोष” (Environment Relief Fund), जो ‘जन उत्तरदायित्व बीमा अधिनियम’ के तहत आता है।
o पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर लगाए गए जुर्माने से मिली राशि।
6. निगरानी और पर्यवेक्षण व्यवस्था
• एक तकनीकी समिति गठित की जाएगी, जिसमें मंत्रालयों, SPCBs, विशेषज्ञों और नियामकों के प्रतिनिधि होंगे।
• यह समिति:
o नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी
o सुधार के सुझाव देगी
o हर साल केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी
7. जनभागीदारी सुनिश्चित
• किसी स्थल को दूषित घोषित किए जाने के 60 दिनों के भीतर लोगों से आपत्तियाँ/सुझाव मँगाए जाएँगे।
• अंतिम सूची स्थानीय अख़बारों में प्रकाशित की जाएगी ताकि जनता को जानकारी मिले।
8. लागत-विभाजन मॉडल
• सफाई में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी इस प्रकार तय की गई है:
o हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 (केंद्र:राज्य)
o अन्य राज्यों के लिए 60:40
o केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र सरकार वहन करेगी
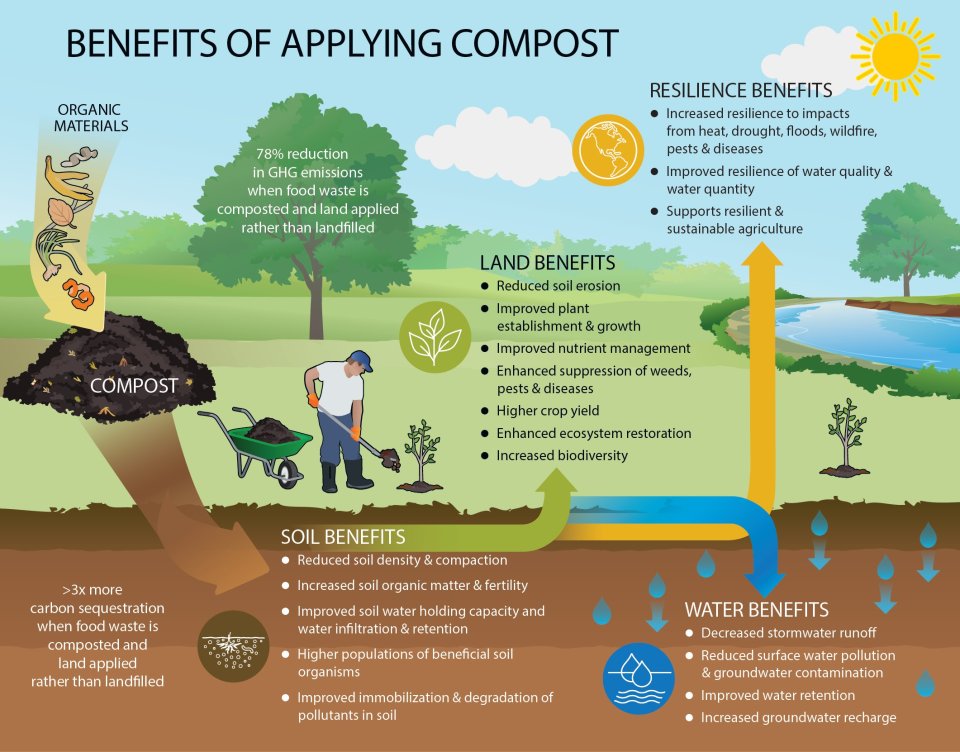
नियमों के लाभ:
• यह नियम दूषित स्थलों की पहचान और सफाई के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित व्यवस्था प्रदान करते हैं, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
• जोखिम-आधारित तरीका उन स्थलों को प्राथमिकता देगा, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सबसे अधिक खतरा बन सकते हैं।
• जनता की भागीदारी और सूचना उपलब्धता से प्रभावित समुदायों को जागरूक और निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा।
नियमों की सीमाएँ:
• ये नियम कुछ विशेष श्रेणियों को बाहर रखते हैं, जैसे कि रेडियोधर्मी कचरे वाले स्थल, खनन क्षेत्र और समुद्री तेल रिसाव, जो अभी भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।
• जहाँ प्रदूषण करने वाला नहीं पहचाना जा सकता, वहाँ सफाई की पूरी लागत वहन करना केंद्र और राज्यों के लिए कठिन हो सकता है।
• इन नियमों की सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी, जो विभिन्न एजेंसियों और हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय के बिना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
निष्कर्ष:
पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 भारत की पर्यावरणीय नीति व्यवस्था में एक बड़ा सुधार है। ऐसे समय में जब देश औद्योगिक प्रदूषण और स्वास्थ्य से जुड़ी पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहा है, ये नियम कानूनी, संस्थागत और तकनीकी स्तर पर एक मजबूत समाधान प्रस्तुत करते हैं। यदि इन्हें ठीक से लागू किया गया, तो यह भारत को स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकते हैं।






