परिचय:
भारत में जीवनशैली में बदलाव, जनसंख्या बढ़ने और पर्यावरणीय कारणों की वजह से कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (NCRP) के अनुसार, भारत में कैंसर के मामले 2020 में 1.39 मिलियन से बढ़कर 2025 तक 1.57 मिलियन हो सकते हैं। हालांकि, इस बढ़ते बोझ के अनुपात में इलाज की व्यवस्था और जनसंख्या-स्तर की निगरानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। विशेष रूप से जल्दी पहचान, रेडियोथेरेपी की उपलब्धता, और डेटा प्रणाली के क्षेत्र में गंभीर खामियां हैं।
· कैंसर एक घातक और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिसके लिए समय पर पहचान और विभिन्न प्रकार के इलाज जरूरी होते हैं। इनमें रेडियोथेरेपी इलाज और दर्द राहत दोनों में अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ ही, एक मजबूत निगरानी प्रणाली का होना जरूरी है ताकि बीमारी का बोझ समझा जा सके, नीतियाँ बनाई जा सकें, संसाधनों का सही आवंटन हो और प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। हालांकि भारत में चार दशकों से कैंसर रजिस्ट्री की कोशिशें जारी हैं, फिर भी रजिस्ट्रियों की पहुंच सीमित है, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में। यह स्थिति तत्काल ध्यान और सुधार की मांग करती है।
भारत में रेडियोथेरेपी की कम पहुंच:
ICMR द्वारा हाल ही में BMC Cancer पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में 58.4% कैंसर मरीजों को इलाज के दौरान किसी न किसी चरण में रेडियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, लेकिन सिर्फ 28.5% को ही यह सुविधा मिलती है। यानी, जिन मरीजों को रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है, उनमें से लगभग आधे को यह नहीं मिल पा रही।
कैंसर के प्रकार के अनुसार यह कमी इस प्रकार है:
- लिम्फोमा: 79.1% की कमी
- फेफड़ों का कैंसर: 69.9%
- प्रोस्टेट कैंसर: 58.5%
- सिर व गर्दन का कैंसर: 44.9%
- गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर: 39.9%
- मस्तिष्क कैंसर: 32%
भारत में कैंसर की पहचान अक्सर देर से होती है, जिससे रेडियोथेरेपी की मांग और बढ़ जाती है। यह तकनीक ट्यूमर को छोटा करने, उसके विकास को नियंत्रित करने और दर्द कम करने में मदद करती है।
रेडियोथेरेपी की कम उपलब्धता के कारण:
इस कमी का मुख्य कारण है – रेडियोथेरेपी मशीनों की भारी कमी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, प्रति दस लाख आबादी पर कम से कम 1 मशीन होनी चाहिए और आदर्श रूप में 4 होनी चाहिए। भारत की आबादी 1.45 अरब है, तो कम से कम 1,450 मशीनों की जरूरत है, जबकि फिलहाल सिर्फ 794 मेगावोल्टेज मशीनें ही हैं।
- हालांकि 2018 से अब तक मशीनों की संख्या में 18% की वृद्धि हुई है (670 से 794), फिर भी ICMR के अनुसार भारत को 1,585 से 2,545 मशीनों की जरूरत है। "लिनियर एक्सेलेरेटर शॉर्टेज इंडेक्स" (LSI) 256 है, जो गंभीर कमी को दर्शाता है।
- अगर कैंसर की जल्द पहचान हो, तो 126 से 222 मशीनों की आवश्यकता को टाला जा सकता है। सिर्फ चार प्रकार के कैंसर – स्तन, गर्भाशय ग्रीवा, सिर व गर्दन, और फेफड़ों – ही 60% रेडियोथेरेपी की मांग के लिए जिम्मेदार हैं।
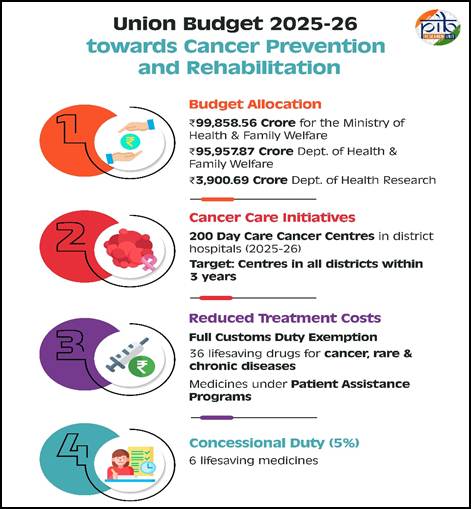
इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए भारत को चाहिए:
- 4,034 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट
- 2,241 मेडिकल फिजिसिस्ट
- 6,732 रेडिएशन थेरेपिस्ट
- अनुमानित निवेश: 64.2 मिलियन से 81.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर
भारत में कैंसर रजिस्ट्री की स्थिति:
- भारत की कैंसर निगरानी प्रणाली कमजोर है। NCRP की शुरुआत 1981 में तीन जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री (PBCRs) और तीन अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्री (HBCRs) के साथ हुई थी। आज यह संख्या 48 PBCRs और 324 HBCRs तक पहुंच गई है, लेकिन कवरेज अभी भी सीमित है।
- PBCRs सबसे बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे किसी क्षेत्र में कैंसर की घटनाओं, मृत्यु दर और प्रवृत्तियों की निगरानी करते हैं। परंतु, ये केवल 18% जनसंख्या और 1% ग्रामीण जनसंख्या को कवर करते हैं।
- HBCRs सिर्फ अस्पताल स्तर पर जानकारी देती हैं और राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर की तस्वीर नहीं देतीं।
- इसका असर यह है कि ग्रामीण, जनजातीय और दूरदराज़ क्षेत्रों की निगरानी नहीं हो पाती, जिससे NPCDCS जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रभावशीलता घट जाती है।
नीति निर्माण में रजिस्ट्री डेटा का उपयोग:
सीमित कवरेज के बावजूद, PBCR डेटा से कई नीतिगत फैसले लिए गए हैं:
- 2024 में HPV वैक्सीन का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार।
- तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों को मजबूत किया गया:
- तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी चित्र
- फिल्मों और टीवी में एंटी-तंबाकू संदेश
- ई-सिगरेट और गुटखा पर रोक
- राष्ट्रीय तंबाकू निवारण हेल्पलाइन
लेकिन जब कवरेज सीमित हो, तो इन प्रयासों का प्रभाव भी सीमित ही रह जाता है।
भारत में कैंसर अब भी ‘नोटिफाएबल डिजीज’ नहीं है?
- कैंसर को भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नोटिफाएबल डिजीज (जिसकी जानकारी देना कानूनी रूप से आवश्यक हो) नहीं माना गया है। यानी अस्पतालों और डॉक्टरों को कैंसर मामलों की जानकारी देने की कानूनी बाध्यता नहीं है।
- हालांकि 15 राज्यों ने इसे नोटिफाएबल घोषित किया है, लेकिन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों ने अब तक ऐसा नहीं किया।
- 2024 में मानवाधिकार आयोग को जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कैंसर एक संक्रामक रोग नहीं है, इसलिए उसे नोटिफाएबल नहीं बनाया जाना चाहिए।
जहां इसे अनिवार्य किया गया है, वहां भी कई समस्याएं बनी हुई हैं:
- कमजोर डिजिटल ढांचा
- पहचान और गोपनीयता की सुरक्षा का अभाव
- डेटा स्टाफ के लिए प्रशिक्षण की कमी
- निजी अस्पतालों द्वारा डेटा साझा करने में अनिच्छा
वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति
भारत कैंसर मामलों की संख्या में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है, लेकिन कैंसर रजिस्ट्री कवरेज के मामले में बहुत पीछे है।
IARC के 2021 डेटा के अनुसार कवरेज:
- उत्तरी अमेरिका: 98%
- ओशिनिया: 77%
- यूरोप: 46%
- एशिया (भारत समेत): 7%
- अफ्रीका: 1%
- वैश्विक औसत: 15%
कुछ उदाहरण:
- अमेरिका: 96% (NPCR), 46% (SEER)
- चीन: ~40% और लगातार बढ़ रही है
- यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया: लगभग 100%
- थाईलैंड और ब्राज़ील: सीमित संसाधनों के बावजूद व्यापक कवरेज
भारत मुंबई से GICR हब के माध्यम से कैंसर रजिस्ट्री प्रशिक्षण का क्षेत्रीय केंद्र है, फिर भी देश में खुद कवरेज बढ़ाने में प्रगति धीमी है।
आगे की राह:
भारत को कैंसर देखभाल और निगरानी के क्षेत्र में तेज़ी से सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिए कई रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं:
1. डिजिटल सिस्टम का लाभ उठाना:
o कैंसर रजिस्ट्री को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) से जोड़ा जाए।
o आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) का उपयोग कर अस्पताल रिकॉर्ड से डेटा संग्रह आसान बनाया जाए।
2. सार्वजनिक-निजी भागीदारी:
o नेशनल कैंसर ग्रिड (NCG) के 360 केंद्र NCRP को सहयोग दें।
o डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रशिक्षण के माध्यम से रजिस्ट्री मजबूत की जा सकती है।
3. कानूनी प्रावधान:
o कैंसर को नोटिफाएबल डिजीज घोषित कर सभी अस्पतालों को रिपोर्टिंग के लिए बाध्य किया जाए।
o डेटा सुरक्षा, प्रशिक्षित कर्मी और मानकीकृत फॉर्मेट लागू किए जाएं।
निष्कर्ष:
भारत कैंसर नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। रेडियोथेरेपी की कम उपलब्धता और निगरानी प्रणाली की कमजोरी को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैंसर के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए भारत को जल्द पहचान, समुचित इलाज और संपूर्ण व डिजिटल निगरानी प्रणाली पर निवेश करना होगा।
जीवनशैली और पर्यावरणीय कारणों से कैंसर के प्रकारों में बदलाव हो रहा है — ऐसे में पुराने और अधूरे आंकड़ों पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। एक मजबूत, समेकित और तकनीकी रूप से सक्षम कैंसर निगरानी प्रणाली अब न केवल आवश्यक है, बल्कि लाखों जानें बचाने के लिए अपरिहार्य भी है।
| मुख्य प्रश्न: कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियों के बढ़ते बोझ के कारण भारत की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं में बदलाव की आवश्यकता है। भारत में कैंसर के उपचार और निगरानी के बुनियादी ढाँचे में मौजूद कमियों के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। |







