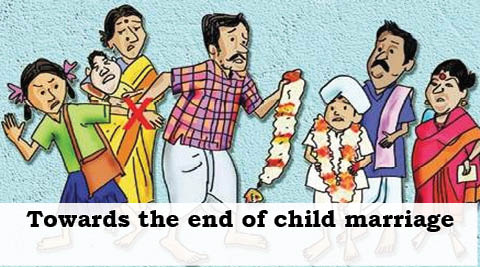सन्दर्भ:
भारत में सख्त कानूनों और व्यापक जागरूकता अभियानों के बावजूद बाल विवाह एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। गहराई से जमी सांस्कृतिक परंपराएँ, गरीबी और लैंगिक असमानता आज भी समय से पहले विवाह को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में कानूनी प्रवर्तन और सामाजिक सुधार को मिलाकर किए गए हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, दक्षिण राजस्थान के जनजातीय बहुल बांसवाड़ा ज़िले ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी व्यवस्था लागू की है—जिसमें किसी भी रिपोर्टेड या संभावित बाल विवाह की स्थिति में न्यायालय से निषेधाज्ञा (injunction) आदेश लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
बांसवाड़ा की नई एसओपी: बाल विवाह रोकने का कानूनी उपाय
बांसवाड़ा ज़िले की 70% से अधिक आबादी जनजातीय समुदायों की है और यह क्षेत्र लंबे समय से उच्च बाल विवाह दर से जूझ रहा है— राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (2019–21) के अनुसार यहाँ बाल विवाह की दर 25% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 23.3% है। इस समस्या से निपटने के लिए, बांसवाड़ा प्रशासन ने यह अनिवार्य कर दिया है कि किसी भी रिपोर्टेड या संदेहास्पद बाल विवाह के मामले में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 13(1) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट से निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करना होगा। यह कानूनी आदेश विवाह को रोकने के लिए बाध्यकारी होता है और इसके उल्लंघन को आपराधिक अपराध माना जाता है।
एसओपी की मुख्य विशेषताएँ
· न्यायालयीय निषेधाज्ञा: अब किसी भी संभावित बाल विवाह की सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी के माध्यम से औपचारिक निषेधाज्ञा आदेश के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
· कानूनी प्रवर्तन: निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। यह मौखिक आश्वासन या लिखित हलफनामे के स्थान पर एक कानूनी रिकॉर्ड तैयार करता है।
· तेज कार्रवाई: पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और एनजीओ की संयुक्त टीमें सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करेंगी।
· विस्तृत दस्तावेज़ीकरण: मजिस्ट्रेट के समक्ष एक पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें नाम, आयु और पारिवारिक विवरण शामिल होंगे।
· प्रशिक्षण और अनुपालन: SOP के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ज़िला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
यह पहल राजस्थान में अपनी तरह की पहली है और यह अनौपचारिक रोकथाम उपायों से हटकर एक कानूनी रूप से प्रभावी रणनीति की ओर संकेत करती है।
भारत में बाल विवाह को समझना:
भारतीय क़ानून के अनुसार, बाल विवाह वह है जिसमें किसी एक पक्ष की आयु- लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष से कम हो। यह प्रथा बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, गरीबी को बनाए रखती है और लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है।
यूनिसेफ़ (2021) के अनुसार:
· भारत में 22.3 करोड़ बाल वधुएँ हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं।
· शहरी क्षेत्रों में दरें घट रही हैं, लेकिन ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में यह समस्या अब भी बनी हुई है।
भारत में बाल विवाह के कारण:
1. गहरी परंपराएँ और पारिवारिक मान-सम्मान
o कई समुदायों में यह विश्वास है कि लड़की की जल्दी शादी करने से परिवार की इज्ज़त बनी रहती है और पूर्व-विवाह संबंधों से बचा जा सकता है।
o सामाजिक रीति-रिवाज़ शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता से ज़्यादा विवाह को प्राथमिकता देते हैं।
2. गरीबी और आर्थिक असुरक्षा
o गरीब परिवारों के लिए शादी खर्च और जिम्मेदारी कम करने का साधन होती है।
o कम उम्र में शादी करने से अक्सर दहेज की मांग भी कम होती है।
3. लैंगिक असमानता
o लड़कियों को अधिकार संपन्न व्यक्ति की बजाय बोझ समझा जाता है।
o पितृसत्तात्मक सोच उनकी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करती है।
4. शिक्षा की कमी
o अशिक्षित परिवारों को बाल विवाह के कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों की जानकारी नहीं होती।
o स्कूल से बाहर लड़कियों के पास सीमित विकल्प होते हैं और वे विरोध भी नहीं कर पातीं।
5. सुरक्षा की चिंता
o परिवार कभी-कभी बेटियों की जल्दी शादी इसलिए कर देते हैं ताकि उन्हें उत्पीड़न या हमले से बचाया जा सके।
6. कानूनों का कमजोर अनुपालन
o कानून होने के बावजूद, कम सज़ा दर, खराब रिपोर्टिंग और प्रशासनिक निष्क्रियता से यह प्रथा जारी रहती है।

बाल विवाह के परिणाम:
· मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य जोखिम:
o कम उम्र की दुल्हनों में गर्भावस्था संबंधी जटिलताएँ और मातृ मृत्यु दर अधिक होती है।
o उनके बच्चों में कुपोषण और कम उम्र में मृत्यु की आशंका ज़्यादा होती है।
· शिक्षा में व्यवधान:
o शादी के बाद लड़कियाँ अक्सर स्कूल छोड़ देती हैं, जिससे उनके रोजगार के अवसर घटते हैं।
· गरीबी का दुष्चक्र:
o शिक्षा की कमी और जल्दी मातृत्व गरीबी को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाता है।
· मानसिक तनाव:
o बाल वधुएँ अक्सर अवसाद और चिंता से ग्रस्त होती हैं।
· घरेलू हिंसा:
o छोटी उम्र की दुल्हनों को शोषण और हिंसा का ज़्यादा खतरा होता है।
· जनसंख्या वृद्धि:
o समय से पहले और बार-बार गर्भधारण से प्रजनन दर अधिक हो जाती है।
भारत में कानूनी ढाँचा:
· बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA):
o वैध विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित करता है।
o विवाह कराने, सहयोग करने या रोकने में असफल रहने वालों को दंडित करता है।
o राज्यों को बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) नियुक्त करने का अधिकार देता है।
· POCSO अधिनियम, 2012:
o नाबालिग के साथ यौन संबंध को बलात्कार की श्रेणी में मानता है।
· शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009:
o स्कूली छोड़ने की दर कम करने के लिए मुफ्त, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।
· दहेज निषेध अधिनियम, 1961:
o दहेज के दबाव को कम करने के लिए लागू किया गया।
सरकारी प्रयास और योजनाएँ:
· बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:
o लड़कियों के जीवन, सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देता है।
· कन्याश्री प्रकल्प (पश्चिम बंगाल):
o स्कूल में बने रहने और विवाह में देरी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देता है।
· अपनी बेटी अपना धन (हरियाणा):
o विवाहित आयु बढ़ाने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण योजना।
· चाइल्डलाइन 1098:
o संकट में बच्चों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन।
· साझेदारियाँ:
o यूनिसेफ और एनजीओ स्थानीय नेताओं और युवा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देकर बाल विवाह को पहचानने और रोकने में मदद करते हैं।
बाल विवाह रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस:
· पूर्णकालिक CMPO की नियुक्ति:
o केवल बाल विवाह की रोकथाम के लिए समर्पित अधिकारी।
· मजिस्ट्रेट को अधिकार:
o मजिस्ट्रेट स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकते हैं।
· फास्ट-ट्रैक कोर्ट:
o बाल विवाह के मामलों के लिए विशेष त्वरित न्यायालय।
· सामुदायिक प्रमाणन:
o गाँवों को "बाल विवाह मुक्त" घोषित किया जा सकता है, जैसे स्वच्छ भारत में "ODF" सर्टिफिकेशन।
· अनिवार्य जवाबदेही:
o कार्रवाई न करने वाले सरकारी कर्मियों को दंडित किया जा सकता है।
तकनीक का उपयोग:
· एक केंद्रीकृत रिपोर्टिंग पोर्टल,
· हाई रिस्क क्षेत्रों की पहचान के लिए डेटा विश्लेषण,
· स्थानीय भाषाओं में डिजिटल जागरूकता अभियान।
वित्त पोषण और क्षमता निर्माण:
· रोकथाम के लिए वार्षिक बजट प्रावधान,
· पुलिस, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण,
· बचाव और पुनर्वास के लिए किशोर न्याय कोष का उपयोग।
निष्कर्ष:
बांसवाड़ा की यह पहल अनौपचारिक उपायों से हटकर कानूनी, दस्तावेज़ीकृत प्रक्रिया की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है, जो अधिकारियों को बाल विवाह को प्रभावी रूप से रोकने में सक्षम बनाती है। यद्यपि कानून और योजनाएँ पहले से मौजूद हैं, लेकिन असली परिवर्तन तभी आता है जब प्रवर्तन को सामुदायिक सहभागिता और सतत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ जोड़ा जाए। ऐसे ही प्रयासों को अन्य उच्च-प्रवण जिलों में लागू कर भारत बाल विवाह समाप्त करने और हर बच्चे के अधिकारों की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है।
यह मॉडल दर्शाता है कि कैसे कानूनी नवाचार, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और सिविल सोसाइटी की साझेदारी मिलकर सामाजिक परिवर्तन ला सकती है।
| मुख्य प्रश्न: बाल विवाह की प्रथा न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में भी बाधा है। इस संदर्भ में, बाल विवाह को रोकने में सामुदायिक सहभागिता और प्रौद्योगिकी की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (250 शब्द) |