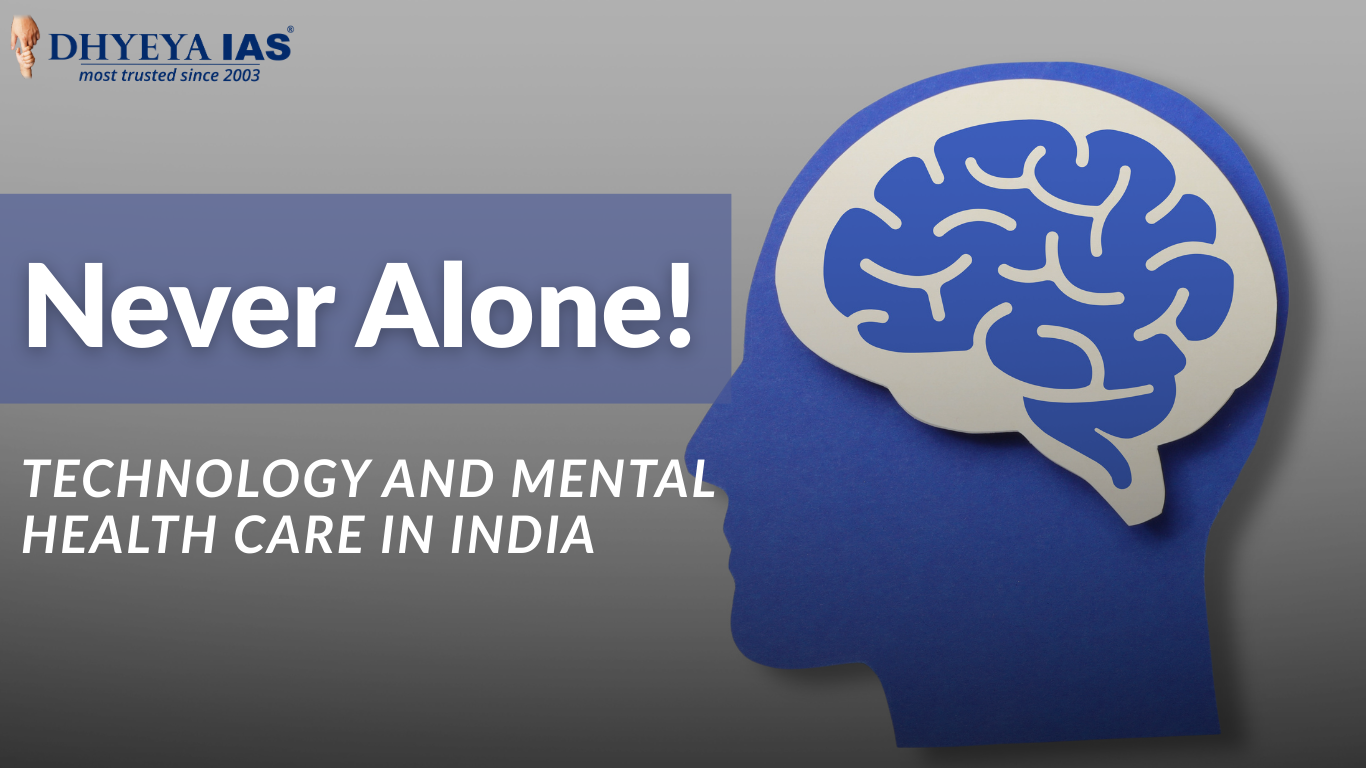संदर्भ
मानसिक स्वास्थ्य भारत में सबसे ज़रूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं में से एक बनकर उभरा है। आँकड़े बेहद गंभीर और चिंताजनक हैं। अकेले 2022 में, देश में आत्महत्या के कारण 1.7 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई, यह आंकड़ा न केवल मनोवैज्ञानिक संकट को दर्शाता है, बल्कि गहरी सामाजिक और आर्थिक कमजोरियों को भी दर्शाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि भारत में विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है, तथा देश में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 2,443 विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (DALYs) का मानसिक स्वास्थ्य बोझ है, जबकि आयु-समायोजित आत्महत्या दर प्रति 100,000 व्यक्तियों पर 21.1 है। मानवीय पीड़ा के अलावा, 2012 से 2030 के बीच मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ी आर्थिक हानि 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान लगाया गया है।
इस पृष्ठभूमि में, मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, विशेष रूप से 2022 में शुरू की गई केंद्र की टेली-मानस पहल, अमूल्य जीवनरेखा रही है। वे संकटग्रस्त लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करते हैं, तथा स्थापना के बाद से अब तक 24 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हो चुकी हैं। राज्य सरकारें और गैर-सरकारी संगठन भी अपनी हेल्पलाइन चलाते हैं। हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि हेल्पलाइनें महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। इन्हें एक व्यापक, व्यवस्थित दृष्टिकोण में एकीकृत किया जाना चाहिए जो मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के विविध स्तरों का समाधान करे। इसी संदर्भ में, भारत सरकार ने हाल ही में 'नेवर अलोन' मानसिक स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया है, जो एक वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है जिसे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को, विशेष रूप से छात्रों के लिए, अधिक सुलभ बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
भारत में मानसिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति प्रसार
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015–16):
- 10.6% वयस्क मानसिक विकारों से पीड़ित हैं।
- आजीवन प्रसार: 13.7%
- हस्तक्षेप की आवश्यकता: वयस्क जनसंख्या का 15%
- शहरी बनाम ग्रामीण: शहरी क्षेत्रों में प्रसार अधिक (13.5%) है जबकि ग्रामीण (6.9%) में कम।
उपचार अंतराल
- 70–92% मानसिक विकारों से पीड़ित लोग उचित उपचार प्राप्त नहीं करते।
- कारण: जागरूकता की कमी, कलंक, पेशेवरों की कमी, और ऊँची लागत।
- मानव संसाधन की कमी: भारत में प्रति 1,00,000 लोगों पर 0.75 मनोचिकित्सक हैं, जबकि WHO की सिफारिश 3 है। इसी प्रकार नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और मनोरोग नर्सों की भी भारी कमी है।
मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक
1. जैविक कारक: मानसिक विकारों का पारिवारिक इतिहास, न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, और पुरानी शारीरिक बीमारियाँ संवेदनशीलता बढ़ाती हैं।
2. मनोवैज्ञानिक कारक: बचपन के आघात जैसे शोषण या उपेक्षा और कुछ व्यक्तित्व लक्षण मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं।
3. पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक कारक: गरीबी, बेरोजगारी, और वित्तीय अस्थिरता तनाव पैदा करते हैं, जबकि आपदाओं, हिंसा या दुर्घटनाओं का संपर्क समस्याओं को बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुँच संकट को और गहरा करती है।
4. जीवनशैली कारक: नशे का दुरुपयोग, खराब आहार, अनियमित नींद और लगातार तनाव मुख्य योगदानकर्ता हैं।
5. सांस्कृतिक और सामाजिक कारक: कलंक, सामाजिक भेदभाव और सांस्कृतिक मान्यताएँ जो मानसिक पीड़ा को कम महत्व या आंकती देती हैं, मदद लेने के व्यवहार को हतोत्साहित करती हैं।
भारत के मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य की प्रमुख चुनौतियाँ
रोगी-केंद्रित चुनौतियाँ
- कलंकित होना: सामाजिक निर्णय के डर से रोगी मदद लेने से बचते हैं।
- उपचार का निरंतर न रहना: दीर्घकालिक परामर्श और थेरेपी बहुत महंगे रहते हैं।
संसाधन संबंधी बाधाएँ
- अस्पताल में बेड: प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर केवल 1.43 मनोरोग बिस्तर।
- पेशेवरों की कमी: प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 0.15 मनोवैज्ञानिक, जबकि सिफारिश 3 की है।
- अनियमित दवा आपूर्ति: खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) स्तर पर।
- पुनर्वास सुविधाएँ: बहुत कम हैं, जिससे रोगियों को दीर्घकालिक देखभाल नहीं मिलती।
प्रशासनिक और संरचनात्मक मुद्दे
- समन्वय की कमी: स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण मंत्रालयों के बीच तालमेल की कमी से दक्षता घटती है।
- धन का कम उपयोग: जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (2015–2020) के तहत राज्यों को आवंटित धन का 40% से कम खर्च किया गया।
- क्षेत्रीय असमानताएँ: ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा होती है क्योंकि पेशेवरों के लिए प्रोत्साहन नहीं हैं।
सरकारी पहलें
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP), 1982
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) एक अग्रणी पहल थी, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए सुलभ और किफायती मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना था। इसका लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान को सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना था।
जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP), 1996
NMHP के तहत शुरू किया गया जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) बेल्लारी मॉडल पर आधारित था। इसका ध्यान प्रारंभिक पहचान और उपचार, सामान्य चिकित्सकों के प्रशिक्षण, जनजागरूकता अभियानों और प्रभावी रिकॉर्ड-कीपिंग और निगरानी पर था।
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017
यह ऐतिहासिक कानून मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार सुनिश्चित करता है। इसके प्रावधानों में शामिल थे:
- आत्महत्या का अपराधीकरण समाप्त करना, इसे स्वास्थ्य मुद्दा मानना।
- व्यक्तियों को अपने उपचार वरीयताओं को निर्दिष्ट करने की अनुमति देने वाले एडवांस डायरेक्टिव्स।
- मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्डों की स्थापना।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अनिवार्य बीमा कवरेज।
- जंजीरों या एकांत जैसे अमानवीय अभ्यासों पर रोक।
टेली-मानस पहल, 2022
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई टेली-मानस देशभर में 24x7 निःशुल्क टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है, खासकर वंचित और दूरदराज़ क्षेत्रों में। यह सबसे बड़ी डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य जीवनरेखाओं में से एक बन गई है, जिसने अपनी शुरुआत से अब तक 24 लाख से अधिक कॉल संभाली हैं।
राज्य और समुदाय-स्तरीय हस्तक्षेप
कर्नाटक
- एन-स्प्राइट (N-SPRITE): आत्महत्या रोकथाम केंद्र, जो शोध, प्रशिक्षण और आत्महत्या रोकथाम रणनीतियों का केंद्र है।
- सुरक्षा प्रोजेक्ट: रामनगर जिले में समुदाय-आधारित आत्महत्या रोकथाम मॉडल।
- उषास प्रोजेक्ट (2022): 11 जिलों के 19 अस्पतालों में आत्महत्या का प्रयास करने वाले 15,623 से अधिक लोगों को परामर्श और सहायता दी गई।
केरल
- जीवनरक्षा कार्यक्रम: “सामुदायिक गेटकीपर्स” को प्रशिक्षित करता है ताकि वे चेतावनी संकेत पहचान सकें, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता दे सकें, और लोगों को पेशेवरों से जोड़ सकें।
- अन्य कार्यक्रमों में प्रसवोत्तर अवसाद के लिए हस्तक्षेप और स्वयंसेवकों के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण शामिल हैं।
तमिलनाडु
- टेली-मानस का स्कूल शिक्षा और सामाजिक कल्याण विभागों की हेल्पलाइन से एकीकरण।
- कक्षा 10वीं, 12वीं और नीट परिणामों के बाद परीक्षा असफलता से परेशान छात्रों तक विशेष पहुँच।
- टेली-मानस जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की डिजिटल शाखा के रूप में भी कार्य करता है, जिससे पहुँच बढ़ती है और कलंक कम होता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 से अंतर्दृष्टि
आर्थिक सर्वेक्षण ने रेखांकित किया कि मानसिक स्वास्थ्य भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश को बनाए रखने में शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य को भावनात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक क्षमताओं को समाहित करने वाला बताया गया और पूरे समुदाय के दृष्टिकोण का आह्वान किया गया।
1. स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करना: छात्रों में चिंता, तनाव और व्यवहार संबंधी समस्याओं की शीघ्र पहचान।
2. कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य नीतियाँ सुधारना: तनाव, लंबे कार्य घंटे और थकान का समाधान।
3. डिजिटल सेवाओं का विस्तार: टेली-मानस को मजबूत करना और एआई-आधारित मानसिक स्वास्थ्य उपकरणों की खोज।
|
नेवर अलोन (Never Alone): मुख्य विशेषताएँ
|
आगे की राह
- उपचार अंतराल को बंद करना: भारत को मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और मनोरोग नर्सों के प्रशिक्षण का विस्तार करना होगा और ग्रामीण तैनाती को प्रोत्साहित करना होगा।
- बुनियादी ढाँचा बढ़ाना: अधिक अस्पताल बिस्तर, पुनर्वास केंद्र, बाह्य रोगी सेवाएँ और नियमित दवा आपूर्ति महत्वपूर्ण हैं।
- प्रशासनिक सुधार: मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय, धन का पूर्ण उपयोग और गाँव स्तर से शुरू होने वाले नीचे-से-ऊपर दृष्टिकोण आवश्यक हैं।
- कलंक का समाधान: बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान, स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता का एकीकरण और सामुदायिक गेटकीपर मॉडल मदद लेने के व्यवहार को सामान्य बना सकते हैं।
- देखभाल को किफायती बनाना: परामर्श लागत को विनियमित करना और बाह्य रोगी देखभाल के लिए व्यापक बीमा कवरेज अनिवार्य करना तुरंत आवश्यक है।
निष्कर्ष
भारत का मानसिक स्वास्थ्य संकट केवल व्यक्तिगत संकट का मामला नहीं है, बल्कि यह व्यवस्थागत, सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का प्रतिबिंब है। आत्महत्याओं और अनुपचारित विकारों की बढ़ती संख्या दर्शाती है कि इस समस्या का समाधान केवल हेल्पलाइन या अस्पतालों के ज़रिए नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामुदायिक हस्तक्षेप और मज़बूत क़ानून से लेकर जागरूकता अभियान और बेहतर संसाधन आवंटन तक, बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
|
मुख्य प्रश्न: मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक एक दोधारी तलवार है। मूल्यांकन कीजिए कि 'नेवर अलोन' ऐप जैसे वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म कैसे छात्रों को सशक्त बना सकते हैं और साथ ही नैतिक/गोपनीयता संबंधी चिंताएँ भी पैदा कर सकते हैं? |