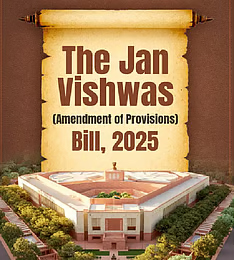परिचय:
वर्षों से भारत की कानूनी और विनियामक प्रणाली में ऐसे अनेक नियम जुड़ते चले गए जो आपराधिक कानून के वास्तविक उद्देश्य से कहीं आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कई प्रावधान शतको पहले, एक बिल्कुल अलग सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य में लिखे गए थे। आज ये अक्सर पुराने, अत्यधिक कठोर या वास्तविक अपराध की तुलना में अनुपातहीन लगते हैं। ऐसे कानूनों की मौजूदगी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जिसमें व्यक्तियों और व्यवसायों को गंभीर सामाजिक हानि वाले कृत्यों के बजाय अनुपालन में त्रुटियों, छोटे डिफॉल्ट्स या प्रक्रियात्मक चूकों जैसी बातों पर भी कारावास का सामना करना पड़ सकता है।
- इस “अति-अपराधीकरण” से कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। यह व्यवसायों के लिए वातावरण को अनिश्चित और जोखिमपूर्ण बनाता है, उद्यमिता को हतोत्साहित करता है और नियामकों पर भरोसा कमजोर करता है। प्रणालीगत स्तर पर, यह भारत की पहले से ही बोझिल न्यायपालिका पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जहाँ लाखों आपराधिक मामले लंबित हैं—जिनमें से कई मामूली अपराधों से जुड़े हैं, जिन्हें सुधारात्मक या वित्तीय दंडों से बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है।
- इस संदर्भ में भारत सरकार ने कानूनी ढाँचे को तार्किक और आधुनिक बनाने के लिए सुधार पहल शुरू की है। जन विश्वास विधेयक इस बदलाव के केंद्र में हैं। पहला विधेयक, 2023 में पारित हुआ, जिसने 42 केंद्रीय कानूनों के तहत 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 अगला बड़ा कदम है। यह 16 और केंद्रीय अधिनियमों में सुधार का विस्तार करता है और निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान लाता है:
• छोटी उल्लंघनों के लिए कारावास की जगह चेतावनी और सुधार नोटिस,
• दंडों का तार्किकीकरण, और
• कारावास के बजाय वित्तीय या सुधारात्मक कार्यवाही पर ध्यान।
जन विश्वास विधेयक लाने का कारण :
भारत का कानूनी ढाँचा बड़ा और जटिल है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा तैयार किए गए डेटाबेस में 882 केंद्रीय कानून दर्ज हैं, जिनमें से 370 में आपराधिक प्रावधान शामिल हैं, जो कुल 7,305 अपराधों को परिभाषित करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से 75% से अधिक अपराध मुख्य आपराधिक न्याय क्षेत्रों के बाहर परिभाषित हैं, जैसे कराधान, शिपिंग, नगर शासन और वित्तीय संस्थान।
अति-अपराधीकरण की लंबे समय से आलोचना की जाती रही है क्योंकि:
- यह अपेक्षाकृत सामान्य या मामूली अपराधों के लिए अनुपातहीन रूप से कठोर दंड निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, भारत में कोई व्यक्ति सड़क पर गाय का दूध निकालने या पालतू कुत्ते को उचित व्यायाम न कराने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है।
- हालाँकि ऐसे प्रावधान शायद ही कभी लागू किए जाते हैं, लेकिन वे अधिकारियों को मनमाने ढंग से शक्ति प्रयोग का अवसर देते हैं।
- ये अपराध और दंड में समानुपातिकता के सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं।
- ऐसे कई कानून पुरानी नैतिक धारणाओं या राज्य की अभिभावक जैसी सोच को दर्शाते हैं।
व्यवसायों पर प्रभाव:
ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन (ORF) की 2022 की एक रिपोर्ट ने भारत में अति-अपराधीकरण के व्यवसायों पर प्रभाव को उजागर किया। रिपोर्ट में पाया गया:
- व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले 1,536 कानूनों में से आधे से अधिक में कारावास की धाराएँ हैं।
- 69,233 अनुपालन आवश्यकताओं में से 37.8% में कारावास का प्रावधान है।
- आधे से अधिक कारावास धाराओं में न्यूनतम एक वर्ष की सजा का प्रावधान है।
रिपोर्ट ने तर्क दिया कि ऐसे प्रावधानों ने पूँजी, विचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन के सहज प्रवाह में बाधाएँ खड़ी की हैं, जिससे अंततः आर्थिक विकास धीमा हुआ है।
न्यायिक प्रणाली पर दबाव:
अत्यधिक अपराधीकरण न्यायपालिका पर बोझ भी बढ़ाता है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, 24 अगस्त 2025 तक भारत की जिला अदालतों में:
- 3.6 करोड़ से अधिक आपराधिक मामले लंबित थे।
- इनमें से 2.3 करोड़ से अधिक मामले एक वर्ष से ज्यादा समय से लंबित थे।
2023 विधेयक की प्रस्तुति के दौरान वाणिज्य मंत्रालय ने उल्लेख किया था कि मामूली डिफॉल्ट्स पर आपराधिक परिणाम न्याय प्रणाली को जाम कर देते हैं और गंभीर मामलों को पीछे धकेल देते हैं, इसलिए अपराधमुक्तिकरण से लंबित मामलों में कमी, अदालतों पर दबाव घटाने और न्याय प्रणाली में सुधार की उम्मीद है।
2025 विधेयक क्या प्रस्तावित करता है?
जन विश्वास विधेयक, 2025 कुल 16 कानूनों में 355 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित करता है। इनमें से:
• 288 प्रावधानों को व्यवसाय सुगमता के लिए अपराधमुक्त किया गया है।
• 67 प्रावधानों में जीवन की सुगमता बढ़ाने के लिए संशोधन किए गए हैं।
विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ:
1. चेतावनी और सुधार नोटिस: विधेयक 10 अधिनियमों के तहत 76 अपराधों में पहली बार अपराध करने वालों के लिए “चेतावनी” और “सुधार नोटिस” का प्रावधान लाता है, जिनमें मोटर वाहन अधिनियम, अपरेंटिस अधिनियम और विधिक मापविज्ञान अधिनियम शामिल हैं।
• उदाहरण: विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत गैर-मानक भार और माप का प्रयोग वर्तमान में ₹1 लाख तक का दंडनीय अपराध है। विधेयक प्रस्तावित करता है कि पहली बार अपराध करने वाले को इसके बजाय सुधार नोटिस दिया जाएगा, जिसमें उसे निर्धारित समय सीमा में गलती सुधारनी होगी। यदि वह पालन करने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माना देना होगा।
2. कारावास धाराओं का हटाना: विधेयक छोटे, प्रक्रियात्मक या तकनीकी डिफॉल्ट्स के लिए कारावास धाराएँ हटाता है। इन्हें जुर्माने या चेतावनी से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
• उदाहरण: विद्युत् अधिनियम, 2003 के तहत आदेशों का पालन न करने पर वर्तमान में तीन माह के कारावास का प्रावधान है। विधेयक प्रस्तावित करता है कि इसे ₹10,000 से ₹10 लाख तक के मौद्रिक जुर्माने से प्रतिस्थापित किया जाए।
3. दंडों का तार्किकीकरण: विधेयक दंडों को अधिक समानुपातिक और पूर्वानुमेय बनाने के लिए तार्किकीकरण करता है। इसमें शामिल हैं:
• हर तीन साल में दंडों में स्वतः 10% वृद्धि, ताकि बिना नए विधायी संशोधन के निवारक शक्ति बनी रहे।
• दोहराए गए अपराधों पर अधिक जुर्माने, ताकि बार-बार उल्लंघन करने वालों को हतोत्साहित किया जा सके और कारावास से बचा जा सके।
जन विश्वास विधेयक के निहितार्थ:
जन विश्वास विधेयक (2023 और 2025) सरकार के बड़े प्रयास का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य भारत की कानूनी संरचना को सरल बनाना और इसे व्यवसाय- और नागरिक-हितैषी बनाना है।
1. व्यवसाय सुगमता: 288 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने से व्यवसायों के लिए अनुपालन जोखिम कम होंगे, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और निवेश बढ़ेगा।
2. जीवन सुगमता: नागरिकों को छोटे उल्लंघनों पर कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे शासन में विश्वास बढ़ेगा।
3. न्यायिक राहत: छोटे अपराधों का अपराधमुक्तिकरण जिला अदालतों पर बोझ कम करेगा और गंभीर अपराधों के लिए न्यायिक समय मुक्त करेगा।
4. नियामक सरलीकरण: दंडों की स्वतः वृद्धि से पूर्वानुमेयता बनेगी और बार-बार संशोधन की आवश्यकता घटेगी।
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:
- निवारण और भरोसे के बीच संतुलन: अपराधमुक्तिकरण से उत्पीड़न कम होता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि अत्यधिक नरमी अनुपालन न करने को प्रोत्साहित कर सकती है।
- कार्यान्वयन चुनौतियाँ: सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नियामक प्राधिकरण कितनी समानता से इसे लागू करते हैं और व्यवसायों व नागरिकों में कितनी जागरूकता फैलाई जाती है।
- अधिक सुधार की आवश्यकता: अभी भी 370 केंद्रीय कानूनों में आपराधिक प्रावधान मौजूद हैं, इसलिए यह केवल एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत है।
जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 भारत के कानूनी तंत्र को आधुनिक बनाने के प्रयास में एक और कदम है। यह 16 अलग-अलग कानूनों में 355 प्रावधानों में बदलाव करता है और महत्वपूर्ण सुधार लाता है, जैसे चेतावनी और सुधार नोटिस, कारावास के स्थान पर मौद्रिक जुर्माना तथा दंडों का तार्किकीकरण। इसका उद्देश्य एक ऐसी शासन प्रणाली का निर्माण करना है जो दंडात्मक होने के बजाय विश्वास-आधारित और नागरिक-हितैषी हो।
|
मुख्य प्रश्न: |