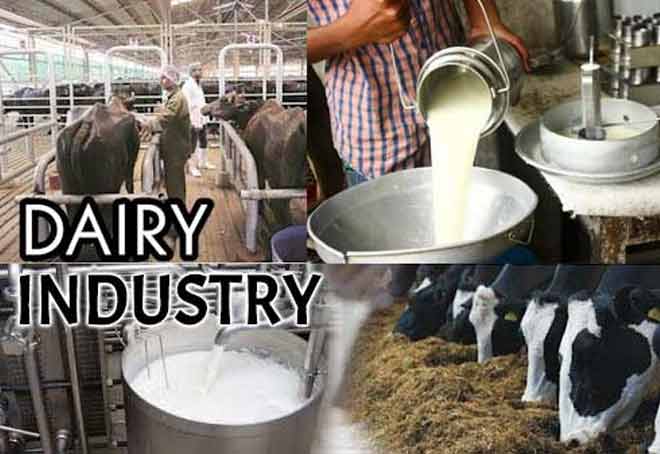परिचय:
- आज भारत 239 मिलियन मीट्रिक टन (2024) दूध उत्पादन के साथ विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है और कुल वैश्विक उत्पादन में लगभग 25% योगदान देता है। कृषि सकल घरेलू उत्पाद (Agricultural GDP) में इसका योगदान लगभग 5% है और 8 करोड़ से अधिक किसान परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी है।
- भारत का यह अद्वितीय मॉडल बड़े औद्योगिक फार्मों पर आधारित नहीं है, बल्कि छोटे किसानों और सीमांत कृषकों द्वारा फसल अवशेषों और उप-उत्पादों से पशुओं को खिलाने की कम लागत प्रणाली पर आधारित है। यही कारण है कि भले ही भारत में प्रति गाय दूध उत्पादन (1.64 टन/वर्ष) अमेरिका (11 टन/वर्ष), यूरोप (7.3 टन/वर्ष) और न्यूजीलैंड (4.6 टन/वर्ष) से बहुत कम हो, फिर भी उत्पादन लागत और बाजार मूल्य की दृष्टि से भारतीय दूध प्रतिस्पर्धी है।
भारत का दुग्ध मॉडल : विशिष्टता और उपलब्धियाँ
भारत का दुग्ध मॉडल अन्य देशों से भिन्न है और यही इसे प्रतिस्पर्धी बनाता है।
1. लघु किसान आधारित उत्पादन प्रणाली
o 50 मिलियन से अधिक छोटे और सीमांत किसान दुग्ध क्षेत्र में सक्रिय हैं।
o अधिकांश किसान 2–3 पशुओं के मालिक होते हैं और दुग्ध आय उनके लिए पूरक आय का साधन है।
2. फसल-अवशेष आधारित चारा
o महंगे पशु-आहार के स्थान पर किसान फसल अवशेष, भूसा, और कृषि-उपोत्पाद का उपयोग करते हैं।
o इससे उत्पादन लागत कम रहती है और किसानों का नकद व्यय घटता है।
3. सहकारी समितियों का नेटवर्क
o अमूल और गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (GCMMF) जैसे मॉडल ने किसानों को बाज़ार से जोड़कर उन्हें अधिक मूल्य उपलब्ध कराया।
o अमूल जैसे सहकारी किसानों को खुदरा मूल्य का 75% से अधिक हिस्सा लौटाते हैं, जबकि अमेरिका में किसानों को केवल 35% मिलता है।
4. महिला सशक्तिकरण और आजीविका
o 80 मिलियन से अधिक किसान परिवार, विशेषकर महिलाएँ, दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हैं।
o स्वयं सहायता समूह (SHGs) और महिला सहकारी समितियाँ आय और सामाजिक स्थिति सुधार में सहायक बनी हैं।
5. मूल्य प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता लाभ
o अमेरिका में 3.5% वसा वाले दूध का मूल्य लगभग ₹36.7 प्रति लीटर (फार्मगेट स्तर) है, जबकि भारत में महाराष्ट्र के किसान को लगभग ₹34 प्रति लीटर मिलता है।
o यूरोप में यही मूल्य ₹55.6 प्रति लीटर है।
o उपभोक्ता स्तर पर अमेरिका में दूध लगभग ₹100 प्रति लीटर बिकता है जबकि अमूल का टोंड मिल्क ₹55–57 में उपलब्ध है।
|
सरकारी पहलें: भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने दुग्ध क्षेत्र के विकास हेतु अनेक योजनाएँ चलाई हैं—
|

चुनौतियाँ : प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की राह में बाधाएँ
1. कम उत्पादकता
o भारत में औसत दूध उत्पादन केवल 1.64 टन प्रति गाय प्रति वर्ष है।
o यह अमेरिका (11 टन) और यूरोप (7.3 टन) की तुलना में बहुत कम है।
2. कम लागत पर आधारित मॉडल की सीमाएँ
o वर्तमान प्रतिस्पर्धा सस्ते और पारिवारिक श्रम पर आधारित है।
o जैसे-जैसे ग्रामीण श्रम महँगा और दुर्लभ होता जा रहा है, यह मॉडल अस्थिर हो रहा है।
3. चारा और पोषण संकट
o उच्च प्रोटीन और पौष्टिक चारे की कमी उत्पादकता को बाधित करती है।
o भारत के पास न्यूजीलैंड जैसी विस्तृत चरागाहें नहीं हैं।
4. रोग और पशु-स्वास्थ्य
o फुट-एंड-माउथ डिजीज (FMD) और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियाँ उत्पादन घटाती हैं।
o पशु-स्वास्थ्य सेवाएँ अभी तक पर्याप्त नहीं हैं।
5. अत्यधिक खंडित उत्पादन संरचना
o अमेरिका केवल 24,470 बड़े फार्मों से दूध उत्पादन करता है, जबकि भारत 50 मिलियन किसानों और 110 मिलियन पशुओं पर निर्भर है।
o इससे पैमाने की अर्थव्यवस्था (Economies of Scale) नहीं बन पाती।
6. प्रसंस्करण और निर्यात की कमी
o केवल 20% दूध ही संगठित प्रसंस्करण क्षेत्र में आता है।
o भारत की वैश्विक निर्यात हिस्सेदारी मात्र 0.3% है।
7. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
o बढ़ती गर्मी और ‘हीट स्ट्रेस’ से पशुओं की प्रजनन क्षमता और दूध उत्पादन प्रभावित हो रहा है।
8. तकनीकी पिछड़ापन
o पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में ऑटोमेशन, IoT, और डिजिटल ट्रैकिंग का उपयोग नगण्य है।
भारत बनाम विश्व : तुलनात्मक परिदृश्य
भारत का मॉडल अभी तक टिकाऊ है, परंतु बदलते समय में केवल सस्ते श्रम पर आधारित प्रतिस्पर्धा टिकाऊ नहीं रह सकती। |
आगे की राह : सुधार और नीतिगत सुझाव
1. नस्ल सुधार और प्रजनन तकनीक
o IVF, एम्ब्रियो ट्रांसफर और जीनोमिक चयन द्वारा उत्पादक नस्लें विकसित करना।
o देशी नस्लों की उच्च-उत्पादक लाइनें तैयार करना।
2. चारा क्रांति
o उच्च प्रोटीन युक्त चारा घास और लेग्युमिनस फसलों की खेती।
o कृषि-अवशेषों के वैज्ञानिक प्रसंस्करण से चारा उपलब्ध कराना।
3. चयनात्मक मशीनीकरण
o छोटे किसानों की सामूहिक समितियों के माध्यम से सस्ती दुग्ध मशीनरी।
o ऊर्जा दक्ष तकनीकों का उपयोग।
4. पशु स्वास्थ्य और टीकाकरण
o ‘वन हेल्थ अप्रोच’ अपनाकर पशु–मानव स्वास्थ्य संबंधी संक्रमणों की रोकथाम।
o मोबाइल वेटरनरी सेवाओं का विस्तार।
5. डिजिटल और स्मार्ट टेक्नोलॉजी
o ब्लॉकचेन आधारित दूध ट्रैकिंग, सेंसर आधारित फीडिंग और स्मार्ट शेड मैनेजमेंट।
o किसान ऐप्स द्वारा बाजार मूल्य और पशु-स्वास्थ्य संबंधी जानकारी।
6. सहकारी नेटवर्क का विस्तार
o अमूल मॉडल को पूरे देश में प्रसारित करना।
o किसानों को उपभोक्ता मूल्य का अधिकतम हिस्सा दिलाना।
7. वैश्विक निर्यात रणनीति
o भारतीय घी, पनीर और दही जैसे उत्पादों को GI टैग और ब्रांडिंग द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतारना।
o FTA वार्ताओं में दुग्ध उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
निष्कर्ष:
भारत का दुग्ध क्षेत्र आजीविका, पोषण और समावेशन का आधार है। यह कृषि के उन चुनिंदा क्षेत्रों में से है जहाँ भारत ने न केवल आत्मनिर्भरता बल्कि वैश्विक दक्षता भी सिद्ध की है परंतु भविष्य की प्रतिस्पर्धा केवल सस्ते श्रम पर आधारित नहीं रह सकती। इसके लिए नस्ल सुधार, पोषण प्रबंधन, तकनीकी नवाचार और चयनात्मक मशीनीकरण आवश्यक हैं। यदि भारत समय रहते सुधारों को लागू करता है, तो न केवल किसानों की आय में स्थायी वृद्धि होगी, बल्कि भारत वैश्विक दुग्ध उद्योग में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकेगा।
| मुख्य प्रश्न : “भारत का दुग्ध क्षेत्र कृषि के उन कुछ क्षेत्रों में से है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बने हुए हैं। किंतु इसकी स्थिरता केवल सस्ते श्रम और पारिवारिक कार्यबल पर आधारित नहीं रह सकती।” इस कथन के आलोक में भारत के दुग्ध क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार, वर्तमान चुनौतियाँ तथा भविष्य के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदमों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द) |