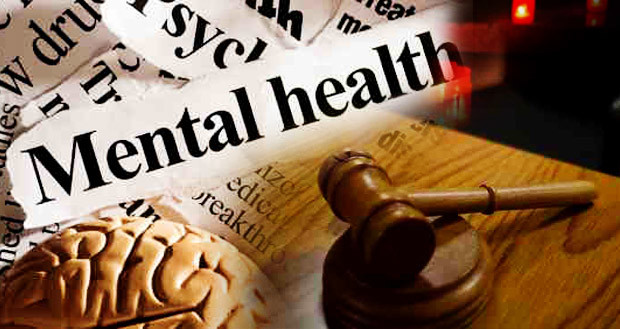सन्दर्भ:
मानसिक स्वास्थ्य, जिसे कभी एक उपेक्षित विषय माना जाता रहा है, अब धीरे-धीरे भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य विमर्श के केंद्र में आ चुका है। हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यह याद दिलाता है कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही आवश्यक है। 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा प्रारंभ किया गया यह दिवस जागरूकता बढ़ाने, कलंक को दूर करने और उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। भारत की यात्रा जो अंधविश्वास और उपेक्षा से शुरू होकर आज के व्यवस्थित सुधारों और डिजिटल नवाचारों तक पहुंची है दुनिया भर के समाजों में मानसिक बीमारियों की समझ और समाधान की विकसित होती सोच को दर्शाती है।
आधुनिक समझ और फ्रायड का प्रभाव:
20वीं शताब्दी में सिग्मंड फ्रायड की मनोविश्लेषण (psychoanalysis) पद्धति ने मानसिक स्वास्थ्य की दिशा ही बदल दी। इसने “टॉक थैरेपी” की अवधारणा दी, जिसने मनोरोग को केवल जैविक व्याख्या से निकालकर अवचेतन भावनाओं और अनुभवों की मनोवैज्ञानिक खोज तक विस्तारित किया।
युद्धोत्तर दशकों में मनोरोग का जैव-चिकित्सीय (biomedical) युग आरंभ हुआ, जिसमें शामिल थे:
-
- विद्युत-आघात चिकित्सा (ECT)
- मनोशल्य चिकित्सा (Psychosurgery)
- मनो-औषध विज्ञान (Psychopharmacology)
लिथियम, वैलियम और प्रोज़ैक जैसी दवाओं ने उपचार में क्रांति ला दी, जिससे लाखों लोग दीर्घकालिक मानसिक विकारों को नियंत्रित कर पाए।
फिर भी, इस युग में दवाओं पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ी, जबकि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू उपेक्षित रहे—यह असंतुलन आज भी विकासशील देशों जैसे भारत में दिखाई देता है, जहाँ जागरूकता, नियमन और परामर्श संरचना अभी भी कमजोर है।
भारत में मानसिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति:
-
- नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे (2015–16), जिसे NIMHANS ने संचालित किया, के अनुसार भारत में लगभग 10.6% वयस्क किसी न किसी मानसिक विकार से पीड़ित हैं। बाद के अध्ययनों के अनुसार, लगभग 15% वयस्कों को पेशेवर हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- शहरी क्षेत्रों में मानसिक विकारों की प्रचलन दर (13.5%) ग्रामीण क्षेत्रों (6.9%) की तुलना में अधिक है—यह अकेलेपन, कार्य तनाव और जीवनशैली से जुड़ी समस्याओं का प्रतिबिंब है।
- द लैंसेट में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी (1990–2017) के अनुसार, 15–49 आयु वर्ग के हर सात में से एक भारतीय मानसिक विकारों से प्रभावित है, जो भारत के गैर-घातक रोगभार का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं।
- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में 2023 में प्रकाशित अध्ययन ने दोहराया कि लगभग 15% भारतीय मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि आत्महत्या युवाओं में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक बनी हुई है।
- महत्वपूर्ण रूप से, आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 ने मानसिक स्वास्थ्य को भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) को बनाए रखने का प्रमुख घटक माना है जिससे मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय उत्पादकता और मानव पूंजी से जोड़ा गया है।
- नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे (2015–16), जिसे NIMHANS ने संचालित किया, के अनुसार भारत में लगभग 10.6% वयस्क किसी न किसी मानसिक विकार से पीड़ित हैं। बाद के अध्ययनों के अनुसार, लगभग 15% वयस्कों को पेशेवर हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
उपचार अंतराल और चुनौतियाँ:
-
- बढ़ती जागरूकता के बावजूद, भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विशाल “ट्रीटमेंट गैप” मौजूद है—70% से 90% तक मानसिक विकारों से पीड़ित लोग किसी औपचारिक उपचार तक नहीं पहुँच पाते। इसके प्रमुख कारण हैं:
- लगातार बना सामाजिक कलंक
- जागरूकता और प्रारंभिक निदान की कमी
- अपर्याप्त अवसंरचना और मानव संसाधन की कमी
- इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री के अनुसार, भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर केवल 0.75 मनोरोग विशेषज्ञ हैं, जबकि WHO की अनुशंसा 3 प्रति 1 लाख है।
मानसिक स्वास्थ्य पर बजट और शोध निवेश अभी भी न्यूनतम है, और सेवाएँ अधिकतर शहरी केंद्रित हैं। - सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ—वर्ग, जाति, शिक्षा और आय से जुड़ी—पहुँच को और सीमित करती हैं। उदारीकरण के बाद की कार्यसंस्कृति, डिजिटल अति-उपयोग और कोविड-19 महामारी ने सभी वर्गों में चिंता, अवसाद और थकान को बढ़ाया है।
- बढ़ती जागरूकता के बावजूद, भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विशाल “ट्रीटमेंट गैप” मौजूद है—70% से 90% तक मानसिक विकारों से पीड़ित लोग किसी औपचारिक उपचार तक नहीं पहुँच पाते। इसके प्रमुख कारण हैं:
सरकारी नीतियाँ और संस्थागत पहलें:
1. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP), 1982
भारत उन शुरुआती विकासशील देशों में था जिसने एक समर्पित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया।
इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत करना और सामुदायिक स्तर तक सेवाएँ पहुँचाना था।
इसका जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) अब 767 जिलों में सक्रिय है, जो प्रदान करता है:
• बाह्य रोगी मनोरोग देखभाल
• परामर्श सेवाएँ
• आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम
• जिला अस्पतालों में 10-बिस्तर वाले वार्ड
2. NIMHANS अधिनियम, 2012
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (NIMHANS), बेंगलुरु को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया।
इससे भारत मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान, शिक्षा और क्षमता निर्माण में अग्रणी बना।
3. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD Act), 2016
1995 के कानून को बदलते हुए, इस अधिनियम में मानसिक बीमारी को विकलांगता की परिभाषा में शामिल किया गया।
यह संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्तियों के अधिकार सम्मेलन (UNCRPD) के अनुरूप है और मानसिक रोगियों को कानूनी सुरक्षा, गरिमा और भेदभाव-मुक्त जीवन का अधिकार देता है।
4. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (MHCA), 2017
यह एक ऐतिहासिक सुधार था, जिसने:
• हर व्यक्ति को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवा का अधिकार दिया
• आत्महत्या को अपराध नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या माना
• मरीज की सहमति, गोपनीयता और सामुदायिक पुनर्वास पर बल दिया
इस अधिनियम के साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास अधिकार-आधारित मानसिक स्वास्थ्य कानून है।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017
इस नीति ने मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया और इसे प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करने की सिफारिश की।
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) के माध्यम से अब जमीनी स्तर पर परामर्श, दवाएँ और रेफरल सेवाएँ उपलब्ध हैं।
6. राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, 2022
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह रणनीति 2030 तक आत्महत्या दर में 10% की कमी का लक्ष्य रखती है।
मुख्य बिंदु:
• प्रारंभिक पहचान और विद्यालय-स्तरीय स्क्रीनिंग
• 24×7 संकट हेल्पलाइन
• उच्च जोखिम समूहों (छात्र, किसान, युवा) के लिए सामुदायिक हस्तक्षेप
7. डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य क्रांति: टेली-मानस
अक्टूबर 2022 में शुरू नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (Tele MANAS) ने भारत को डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य के युग में प्रवेश कराया।
यह 14416 / 1800-89-14416 टोल-फ्री नंबरों के माध्यम से 20 भारतीय भाषाओं में 24×7 मुफ्त सहायता प्रदान करता है।
फरवरी 2025 तक:
• 1.8 मिलियन से अधिक कॉल संभाले गए
• 53 टेली-MANAS सेल, 23 मेंटरिंग संस्थान और 5 क्षेत्रीय केंद्र सक्रिय
• 2024 में टेली-MANAS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसमें स्व-देखभाल, तनाव प्रबंधन और वीडियो परामर्श की सुविधाएँ हैं।
WHO ने टेली-MANAS को समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य का समावेशी और विस्तार योग्य मॉडल माना है। इसने पहले के किरण हेल्पलाइन (2020) को भी इसमें समाहित किया है।
8. क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास
मानव संसाधन की कमी को दूर करने हेतु:
• 25 उत्कृष्टता केंद्र और 47 स्नातकोत्तर मानसिक स्वास्थ्य विभाग स्थापित किए गए हैं।
• iGOT-Diksha प्लेटफॉर्म के माध्यम से डॉक्टरों, नर्सों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं को मानसिक विकारों की पहचान और उपचार हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25: मानसिक स्वास्थ्य एक मानव पूंजी के रूप में:
सर्वेक्षण ने रेखांकित किया कि मानसिक स्वास्थ्य उत्पादकता और आर्थिक विकास की आधारशिला है।
मुख्य सिफारिशें:
• विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा शामिल की जाए ताकि प्रारंभिक स्तर पर सहनशीलता विकसित हो।
• कार्यस्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य नीति लागू की जाए ताकि बर्नआउट और लंबे कार्य घंटों से निपटा जा सके।
• टेली-MANAS और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाए।
मानसिक स्वास्थ्य को मानव पूंजी के स्तंभ के रूप में स्थापित करते हुए, भारत ने उपचार-आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर निवारक और सामुदायिक देखभाल पर जोर दिया है।
निष्कर्ष:
भारत की मानसिक स्वास्थ्य यात्रा उसके व्यापक सामाजिक विकास का प्रतिबिंब है। प्राचीन समग्र ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा और डिजिटल पहुंच के साथ जोड़कर, भारत एक दयालु और समावेशी मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। एक ऐसा राष्ट्र जो मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, वह न केवल स्वस्थ नागरिक बनाता है, बल्कि एक अधिक संवेदनशील और लचीला समाज भी निर्मित करता है।
| UPSC/PSC मुख्य प्रश्न: “मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 जैसे प्रगतिशील कानूनों और बढ़ती जागरूकता के बावजूद, भारत की मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली अभी भी संरचनात्मक और सामाजिक बाधाओं का सामना कर रही है।” चर्चा करें। |