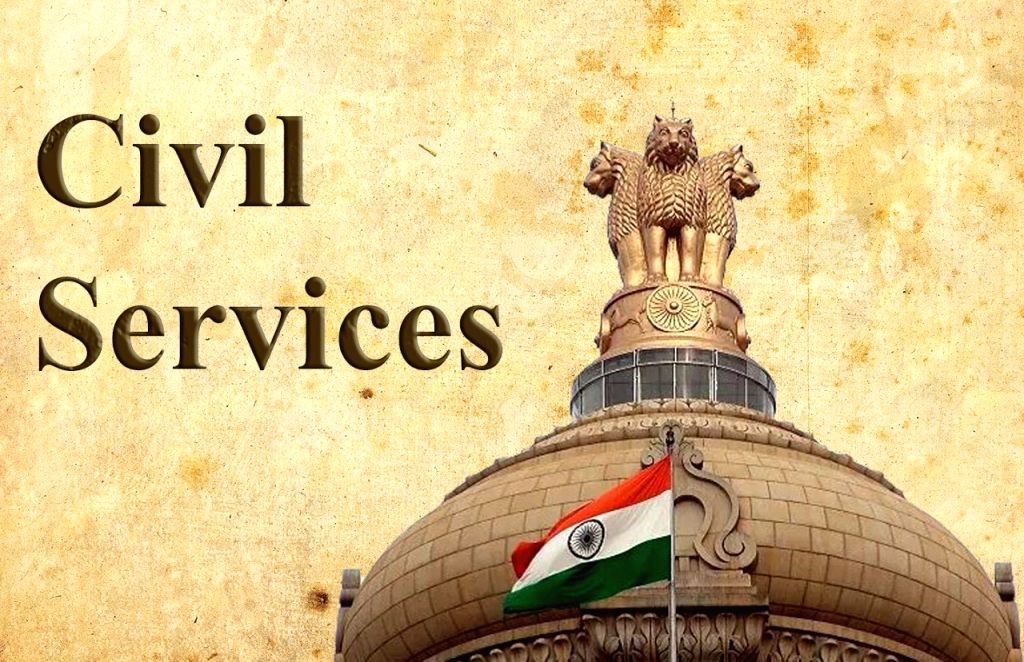संदर्भ:
सिविल सेवाएं भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। जहां निर्वाचित प्रतिनिधि प्रत्येक चुनाव चक्र के साथ बदलते रहते हैं, वहीं सिविल सेवक जिन्हें स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है निरंतरता, स्थिरता और निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करते हैं। कानूनों को लागू करने और जन सेवाएं प्रदान करने की अहम जिम्मेदारी के साथ, सिविल सेवाएं राष्ट्र-निर्माण, सामाजिक-आर्थिक विकास और नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 21वीं सदी में शासन से जुड़ी जटिल चुनौतियों से जूझते भारत के लिए सिविल सेवाओं की प्रासंगिकता और प्रदर्शन, देश की लोकतांत्रिक और विकासात्मक आकांक्षाओं के केंद्र में है।
सिविल सेवाओं की मूल जिम्मेदारियां-
- सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन: सिविल सेवक विधायी इरादों को व्यावहारिक परिणामों में बदलते हैं। विस्तृत कार्यान्वयन ढांचे तैयार करने से लेकर विभागों के बीच समन्वय करने तक, वे पीएमएवाई, मनरेगा या डिजिटल इंडिया जैसी प्रमुख योजनाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं।
- शासन की निरंतरता सुनिश्चित करना: गैर-राजनीतिक अधिकारियों के रूप में, सिविल सेवक संस्थागत स्मृति प्रदान करते हैं। सरकार बदलने, राष्ट्रपति शासन लागू होने या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी वे प्रशासनिक कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रखते हैं।
- नीति निर्माण और प्रारूपण में योगदान: वरिष्ठ सिविल सेवक विशेषज्ञ सलाह देने, विधेयकों का मसौदा तैयार करने और कैबिनेट नोट तैयार करने जैसे कार्यों के माध्यम से नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनका क्षेत्रीय अनुभव और प्रशासनिक अंतर्दृष्टि प्रमुख विधानों की रूपरेखा को आकार देती है।
- सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: सिविल सेवक विकास योजनाओं की निगरानी करते हैं, कल्याणकारी योजनाएं लागू करते हैं और समावेशी विकास के संकेतकों का मूल्यांकन करते हैं। वे विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- आपदा और संकट प्रबंधन: प्राकृतिक आपदाओं से निपटना हो, महामारी का जवाब देना हो या सांप्रदायिक अशांति के दौरान व्यवस्था बहाल करना हो—सिविल सेवक पहले प्रतिक्रिया देने वालों के रूप में कार्य करते हैं। संकट की स्थितियों में उनका नेतृत्व सरकारी प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता तय करता है।
- कानून-व्यवस्था बनाए रखना: भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और जिला स्तर पर कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, कानून लागू करने और पुलिसिंग तथा मजिस्ट्रेटीय कार्यों के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में कार्यरत होते हैं।
- प्रशासनिक न्यायिक कार्य: जिला मजिस्ट्रेट, आयुक्त या न्यायाधिकरण सदस्य के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य करते हुए सिविल सेवक अर्ध-न्यायिक भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे कि प्रशासनिक विवादों का निपटारा, स्वीकृतियां देना और दावों का निवारण करना।
- नैतिक शासन को बनाए रखना: सिविल सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे संवैधानिक मूल्यों का पालन करें, भय या पक्षपात के बिना कार्य करें और सार्वजनिक कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा दें।
भारत में सिविल सेवाओं का संरचनात्मक वर्गीकरण:
1. अखिल भारतीय सेवाएं (AIS): इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFoS) शामिल हैं। इन अधिकारियों की भर्ती केंद्र द्वारा की जाती है, लेकिन वे केंद्र और राज्यों दोनों में कार्य करते हैं, जिससे संघीय ढांचे में प्रशासनिक एकरूपता बनी रहती है।
2. केंद्रीय सिविल सेवाएं: ये अधिकारी पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं, जैसे भारतीय राजस्व सेवा (IRS), भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा (IA&AS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और अन्य विभाग।
3. राज्य सिविल सेवाएं: इनकी भर्ती संबंधित राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा की जाती है और ये अधिकारी अपने-अपने राज्यों की प्रशासनिक संरचना में कार्य करते हैं।
सिविल सेवाओं को ‘स्थायी कार्यपालिका’ क्यों कहा जाता है?
राजनीतिक कार्यपालिका के विपरीत, जो एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होती है, सिविल सेवक सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बने रहते हैं। यह स्थायित्व प्रशासनिक स्थिरता प्रदान करता है और राष्ट्रीय लक्ष्यों के दीर्घकालिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। लगातार बदलती सरकारों के बीच सेतु के रूप में कार्य करते हुए, सिविल सेवक विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, शासन में तटस्थता बनाए रखते हैं और राजनीतिक बदलाव के बीच निरंतरता सुनिश्चित करते हैं।
सिविल सेवाओं के सामने चुनौतियां:
- राजनीतिक तटस्थता का क्षरण: सिविल सेवकों को अब बढ़ती संख्या में राजनीतिक हितों के साथ संरेखित होते हुए देखा जा रहा है, जिससे उनके नीति के निष्पक्ष क्रियान्वयन की संवैधानिक भूमिका कमजोर होती है।
- तैनातियों में राजनीतिक हस्तक्षेप: राजनीतिक कारणों से बार-बार किए जाने वाले तबादले नीतिगत निरंतरता को बाधित करते हैं और अधिकारियों का मनोबल गिराते हैं।
- जनरलिस्ट प्रभुत्व: स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और वित्त जैसे जटिल क्षेत्रों का प्रबंधन करने के बावजूद, कई सिविल सेवकों के पास क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण का अभाव होता है। यह जनरलिस्ट दृष्टिकोण प्रमाण-आधारित नीति निर्माण को बाधित करता है।
- भ्रष्टाचार और लालफीताशाही: निर्णय लेने में देरी, प्रक्रियागत अड़चनें और जवाबदेही की कमी ने इस प्रणाली को अकार्यक्षमता और भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील बना दिया है।
- प्रौद्योगिकी का अपर्याप्त उपयोग: ई-गवर्नेंस पहलों के विस्तार के बावजूद, कई विभाग अभी भी पुराने प्रक्रियाओं से संचालित होते हैं और डिजिटल परिवर्तन का विरोध करते हैं।
योग्यता आधारित प्रणाली बनाम उपहार आधारित प्रणाली: भारतीय संदर्भ
भारत एक योग्यता-आधारित भर्ती प्रणाली का पालन करता है, जो मुख्यतः यूपीएससी के माध्यम से सुनिश्चित होती है, जिसके तहत सिविल सेवकों का चयन कठोर परीक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है। इसके विपरीत, उपहार प्रणाली, जिसे अतीत में अमेरिका जैसे देशों में अपनाया गया था, राजनीतिक नेताओं को वफादारों की नियुक्ति करने की अनुमति देती थी, जो अक्सर प्रशासनिक दक्षता की कीमत पर होता था। भारत ने उपहार प्रणाली को बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया है, लेकिन बढ़ती राजनीतिक नियुक्तियों और लैटरल एंट्री को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि योग्यता आधारित व्यवस्था बनी रहे।
हाल की सरकारी पहलें और सुधार:
- लैटरल एंट्री योजना: कृषि, वित्त और वाणिज्य जैसे मंत्रालयों में संयुक्त सचिव स्तर पर क्षेत्र विशेषज्ञों को लाने के लिए शुरू की गई।
- मिशन कर्मयोगी: एक क्षमता-निर्माण कार्यक्रम जो सिविल सेवकों के कौशल को निरंतर प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से सुधारने के उद्देश्य से शुरू किया गया।
- प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन: मूल्यांकन प्रणाली का डिजिटलीकरण और प्रमुख परिणाम क्षेत्रों (KRAs) पर ध्यान केंद्रित कर अधिकारियों की प्रभावशीलता का आकलन।
- निर्धारित कार्यकाल नीति: मनमाने तबादलों को कम करने और प्रशासनिक भूमिकाओं में स्थिरता लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- केंद्रीय प्रतिनियोजन को सुव्यवस्थित करना: विभिन्न सेवाओं के बीच केंद्रीय पोस्टिंग को अधिक समावेशी बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।
आगे की राह:
- स्वायत्तता को मजबूत करना: राजनीतिक दबाव से नौकरशाहों की रक्षा के लिए संस्थागत तंत्र विकसित किए जाने चाहिए।
- क्षेत्रीय विशेषज्ञता: अधिकारियों को क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और दीर्घकालिक विशेषज्ञता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- प्रौद्योगिकी को अपनाना: डेटा-आधारित शासन और एआई-समर्थित नीति उपकरणों को मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए।
- परिणाम आधारित शासन: मूल्यांकन फाइलों की गति के बजाय सामाजिक प्रभाव और सेवा वितरण पर आधारित होना चाहिए।
- विविधता और समावेशन को बढ़ावा देना: कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों और लैंगिक समानता से जुड़ी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना एक संस्थागत लक्ष्य होना चाहिए।
निष्कर्ष-
भारतीय सिविल सेवाएं लंबे समय से लोकतांत्रिक शासन की एक मजबूत आधारशिला रही हैं, जो विकास, समता और प्रशासनिक निरंतरता की प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच संतुलन बनाए रखती हैं। हालांकि, जैसे-जैसे भारत वैश्वीकरण, डिजिटल व्यवधान और नागरिक जागरूकता से चिह्नित अधिक जटिल शासन परिदृश्य की ओर बढ़ रहा है, सिविल सेवाओं को संरचनात्मक और सांस्कृतिक सुधार की आवश्यकता है। तटस्थता सुनिश्चित करना, व्यावसायिक क्षमता बढ़ाना और नवाचार को प्रोत्साहित करना अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। एक भविष्य-उन्मुख, नागरिक-केंद्रित और उत्तरदायी सिविल सेवा ही ‘नए भारत’ की आकांक्षाओं को साकार कर सकती है।
| मुख्य प्रश्न: “जहां एक ओर सिविल सेवाएं शासन में निरंतरता प्रदान करती हैं, वहीं इनकी सामान्यवादी दृष्टिकोण अक्सर नीति की दक्षता को सीमित कर देती है।” उपयुक्त उदाहरणों सहित इस कथन की विवेचना कीजिए। |