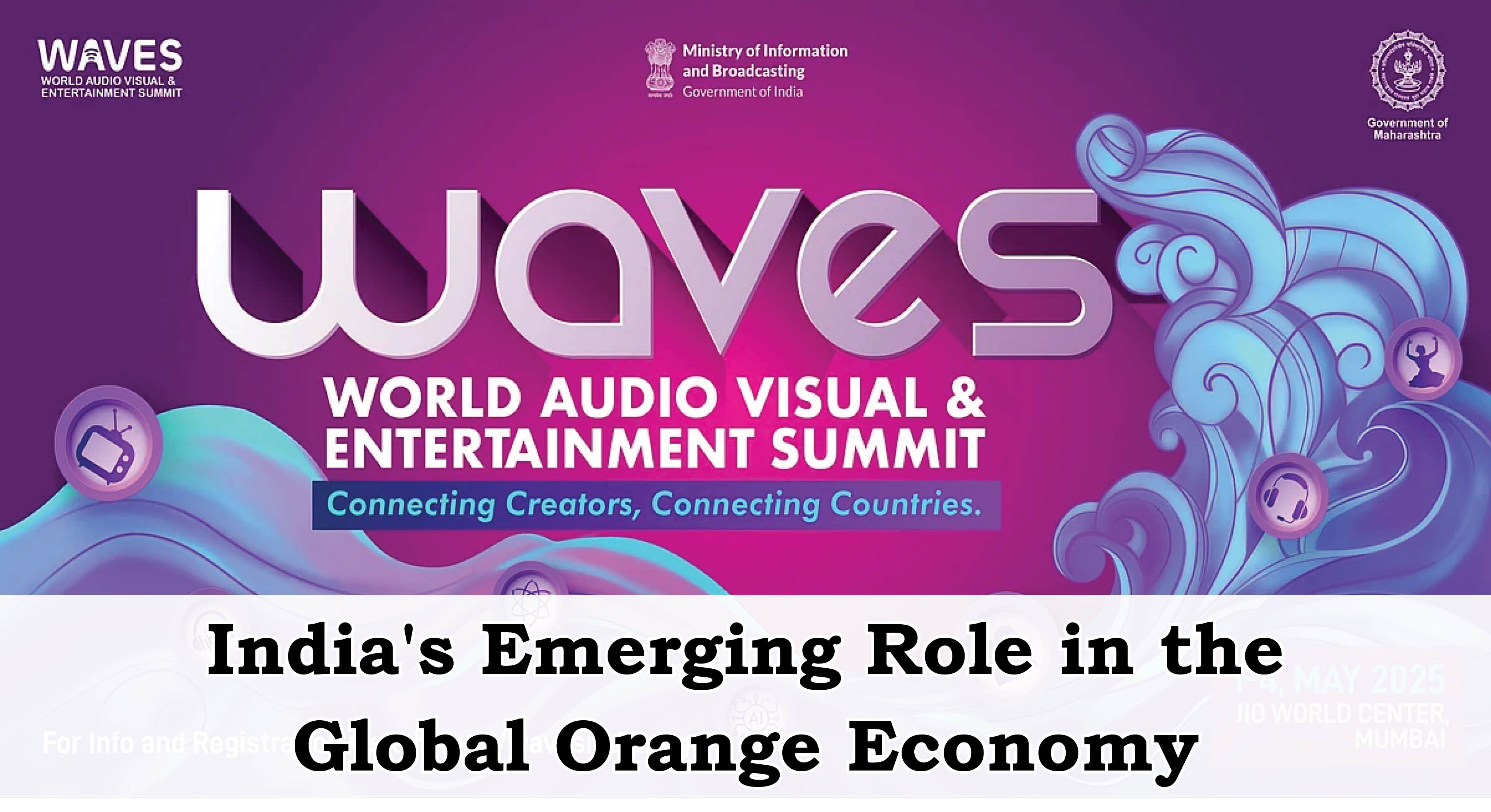भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था (जिसे "ऑरेंज इकॉनमी" भी कहा जाता है) अब सॉफ्ट पावर, राष्ट्रीय ब्रांडिंग और सामाजिक-आर्थिक विकास के एक शक्तिशाली रूप में उभर रही है। इसमें सिनेमा, संगीत, कला, फैशन, डिजाइन, साहित्य, वास्तुकला, हस्तशिल्प, डिजिटल कंटेंट और गेमिंग जैसे कई रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं। यह अर्थव्यवस्था संस्कृति, रचनात्मक सोच और व्यापार के मिलन को दर्शाती है। इसकी क्षमता न केवल इसके आर्थिक योगदान में निहित है, बल्कि कथाओं को आकार देने, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बनाने और भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करने में भी निहित है।
- मुंबई में हुए विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपने नागरिकों को बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने वैश्विक रचनाकारों को संबोधित करते हुए संदेश दिया: “भारत में सृजन करें, विश्व के लिए सृजन करें।” उनका यह संदेश दिखाता है कि भारत वैश्विक ऑरेंज इकॉनमी में अपनी जगह और मज़बूत करना चाहता है। यह क्षेत्र रचनात्मकता, बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) और सांस्कृतिक नवाचार से चलता है।
- प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी बताया कि भारत हमेशा से विविध संस्कृतियों को अपनाने वाला देश रहा है, जैसे पारसी और यहूदी समुदायों का भारत में शांतिपूर्ण मिलन। उन्होंने भारत को एक उभरती हुई ऑरेंज इकॉनमी बताया, जो सिर्फ कला और अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक तरक्की, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संवाद में भी अहम भूमिका निभा रही है।
ऑरेंज अर्थव्यवस्था के बारे में:
सबसे पहले लैटिन अमेरिका में प्रचलित शब्द "ऑरेंज इकोनॉमी" अब दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। वर्तमान में यह रचनात्मकता, प्रतिभा और बौद्धिक संपदा में निहित उद्योगों को संदर्भित करता है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, रचनात्मक अर्थव्यवस्था वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 3% से अधिक का योगदान देती है और दुनिया भर में 30 मिलियन से अधिक नौकरियों का योगदान देती है। भारत में, इस क्षेत्र का योगदान लगभग 160 बिलियन डॉलर (जीडीपी का लगभग 7%) होने का अनुमान है और यह सालाना 10% से अधिक की दर से बढ़ रहा है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं।
भारत की ताकत इसकी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत, तेज़ी से बढ़ती डिजिटल क्षमताओं, युवा आबादी और लोक कलाओं से जुड़े बड़े अनौपचारिक क्षेत्र में छिपी है। देश भर में यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था कई रूपों में देखने को मिलती है — जैसे बेंगलुरु के डिज़ाइन स्टार्टअप्स, दिल्ली के फैशन हब, पुणे के एनिमेशन स्टूडियो, और कच्छ के पारंपरिक कारीगर। यह क्षेत्र पुराने पारंपरिक ज्ञान और नए आधुनिक विचारों का मेल है, जो भारत की विशिष्ट पहचान को दर्शाता है।
सिनेमा के ज़रिए भारत की वैश्विक सांस्कृतिक पहचान:
भारत की ऑरेंज इकॉनमी का सबसे प्रमुख और दृश्य रूप सिनेमा है, जिसे भारत का सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक निर्यात माना जाता है। भारत हर साल 20 से अधिक भाषाओं में 2000 से ज़्यादा फिल्में बनाता है, जिससे वह दुनिया का सबसे बड़ा फ़िल्म-निर्माता देश बन चुका है। भारतीय सिनेमा “चाहे वह बॉलीवुड हो, टॉलीवुड, कॉलीवुड या अन्य क्षेत्रीय फिल्में” केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भारतीय मूल्यों, कहानियों और सौंदर्यशास्त्र का वैश्विक प्रतिनिधि भी है।
ऑस्कर जीतने वाला गाना नाटू-नाटू, कान्स फिल्म फेस्टिवल में मिली पहचान और आरआरआर, दंगल और लगान जैसी फिल्मों की अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता यह दिखाती है कि भारतीय सिनेमा वैश्विक दर्शकों को कितनी गहराई से प्रभावित कर रहा है। नेटफ्लिक्स और अमेज़ॅन प्राइम जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स ने भारतीय कहानियों को दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचाने की रफ्तार और बढ़ा दिया है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में क्षेत्रीय सिनेमा का उभरना इस बात का संकेत है कि भारत की पहचान अब सिर्फ एक भाषा या शैली तक सीमित नहीं, बल्कि वह एक बहुभाषी, विविध और समावेशी सांस्कृतिक ताकत बनकर उभर रही है। हालांकि, यह भी समझना जरूरी है कि सिनेमा रचनात्मकता के इस विशाल समुंदर का केवल एक सिरा है, इसके नीचे और भी गहराई व संभावनाएं छुपी हुई हैं।
स्क्रीन से आगे भारत का व्यापक रचनात्मक परिदृश्य:
भारत की ऑरेंज इकॉनमी में कई ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो देश की “ऐतिहासिक विरासत और आज की रचनात्मक ऊर्जा” दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं:
- संगीत और प्रदर्शन कलाएँ: भारत का संगीत संसार शास्त्रीय परंपराओं से लेकर आधुनिक इंडी फ्यूज़न (यह कलाकार पारंपरिक भावनाओं को आधुनिक साउंड के साथ मिलाते हैं) तक फैला है। यूट्यूब, स्पॉटिफाई (Spotify) और कोक स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म भारतीय संगीत को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं और इसे अधिक लोकप्रिय बना रहे हैं।
- डिज़ाइन और वास्तुकला: भारतीय डिज़ाइनर पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक, टिकाऊ डिज़ाइनों में ढाल रहे हैं। जयपुर को यूनेस्को द्वारा शिल्प और लोककला के रचनात्मक शहर का दर्जा मिला है, जबकि अहमदाबाद को वास्तुकला के लिए विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है।
- फैशन: भारत का वस्त्र और फैशन क्षेत्र, खासतौर पर हथकरघा और खादी पर आधारित डिज़ाइन, अब दुनिया भर में सतत (सस्टेनेबल) और जागरूक फैशन की अगली कड़ी बन चुका है। कई प्रसिद्ध डिज़ाइनर भारतीय सौंदर्यबोध को अंतरराष्ट्रीय रनवे पर प्रस्तुत कर रहे हैं।
- गेमिंग और एनिमेशन: भारत का गेमिंग उद्योग 2027 तक 8.6 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की ओर अग्रसर है। स्वदेशी पात्र, पौराणिक कथाओं और AR/VR तकनीकों के ज़रिए नई कहानियाँ और अनुभव रचे जा रहे हैं।
- साहित्य और प्रकाशन: अरुंधति रॉय, अरविंद अडिगा और गीतांजलि श्री जैसे लेखकों की बुकर पुरस्कार विजित कृतियों के ज़रिए भारत की साहित्यिक आवाज़ अब वैश्विक विमर्श को प्रभावित कर रही है। साथ ही, भारतीय भाषाओं में लिखा साहित्य अब अनुवादों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा और सराहा जा रहा है।
- डिजिटल इन्फ्लुएंसर संस्कृति: सोशल मीडिया क्रिएटर्स, डिजिटल कलाकार और यूट्यूबर्स आज की ऑरेंज इकॉनमी में सूक्ष्म उद्यमियों की एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, विशेष रूप से जनरेशन जेड (Gen Z) के बीच यह रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है।
प्रवासी समुदाय की भूमिका और वैश्विक सहभागिता:
भारत का 32 मिलियन का प्रवासी समुदाय इसके रचनात्मक निर्यात को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कारक है। विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्य उत्सव, फिल्म स्क्रीनिंग और कला प्रदर्शनियाँ भारतीय परंपराओं को जीवित रखती हैं और साथ ही अंतर-सांस्कृतिक संवादों को आमंत्रित करती हैं। यू.के., यू.एस., यू.ए.ई. और कनाडा में, भारतीय रचनात्मक - चाहे वह सिनेमा में मीरा नायर हों या रूपी कविता में कौर के योगदान ने वैश्विक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को आकार दिया है।
इसके अलावा, वैश्विक कलाकारों और मंचों के साथ सहयोग बढ़ा है। भारतीय डिजाइनर वैश्विक लक्जरी ब्रांडों के साथ काम कर रहे हैं; भारतीय संगीत अंतरराष्ट्रीय विज्ञापनों और प्लेलिस्ट का हिस्सा है; भारतीय वास्तुकला फर्म विदेशों में निर्माण कर रही हैं। यह अंतरराष्ट्रीय रचनात्मक आंदोलन भारत के वैश्विक प्रभाव को राजनीतिक दबाव के माध्यम से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अपील के माध्यम से बढ़ाता है।
नीति में अंतराल और विकास की संभावनाएँ:
भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था जितनी जीवंत और संभावनाओं से भरी हुई है, उतनी ही उसे एक संगठित और दूरदर्शी नीति की आवश्यकता है। फिलहाल, इसमें दक्षिण कोरिया के 'हल्लु' (कोरियन वेव) मॉडल या यूनाइटेड किंगडम की रचनात्मक उद्योग नीति जैसी एक ठोस राष्ट्रीय रणनीति का अभाव है। नीति के स्तर पर बिखराव, बड़ी संख्या में अनौपचारिक कार्यबल, बौद्धिक संपदा (IP) की सुरक्षा में कमजोर प्रवर्तन और सीमित निर्यात सहायता जैसे कारक इसके विकास की गति और स्थायित्व में बाधा बनते हैं।
हस्तक्षेप के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
- रचनात्मक अवसंरचना : रचनात्मक केन्द्र, स्टूडियो, सह-कार्यशील स्थान और डिजिटल इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना करना ।
- नीतिगत प्रोत्साहन : कर छूट, निर्यात प्रोत्साहन, तथा सांस्कृतिक उद्यमियों और रचनात्मक स्टार्टअप के लिए अनुदान।
- कौशल एवं शिक्षा : कला और डिजिटल रचनात्मकता को मुख्यधारा की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में एकीकृत करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्माण : द्विपक्षीय सांस्कृतिक समझौते, सह-निर्मित फिल्में और विनिमय कार्यक्रम।
- डेटा और मापन : नीति बनाने के लिए रचनात्मक क्षेत्र के आर्थिक योगदान पर बेहतर नज़र रखना।
संस्कृति मंत्रालय और नीति आयोग ने रचनात्मक उद्योगों को समर्थन देने के लिए रूपरेखाओं की खोज शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, मेकांग-गंगा सहयोग, भारत-अफ्रीका सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जी-20 सांस्कृतिक एजेंडा जैसी पहल भारत की ऑरेंज अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करने और उससे पैसा कमाने के लिए कूटनीतिक रास्ते प्रदान करती हैं।
क्रिएटिव सॉफ्ट पावर का रणनीतिक महत्व:
21वीं सदी में प्रभाव और वैश्विक स्थिति तय करने में सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर जितनी ही प्रभावशाली साबित हो रही है। आकर्षक कहानियाँ गढ़ने, सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने और भावनात्मक जुड़ाव बनाने की क्षमता अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक केंद्रीय तत्व बन चुकी है। भारत की ऑरेंज इकॉनमी यही सामर्थ्य प्रदान करती है, ऐसी शक्ति जो दबदबे के बजाय संवाद और सहयोग पर आधारित है।
रचनात्मक क्षेत्रों में निवेश के ज़रिए भारत न केवल करोड़ों युवाओं को रोज़गार और आत्मनिर्भरता के अवसर दे रहा है, बल्कि वैश्विक चेतना में खुद को एक ऐसे देश के रूप में पुनःस्थापित भी कर रहा है जो नवाचार, विविधता, आत्मा और लचीलापन का प्रतीक है।
निष्कर्ष:
भारत की ऑरेंज इकॉनमी केवल एक सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता है। यह न केवल नए रोज़गार के अवसर पैदा करने और समुदायों को सशक्त बनाने की क्षमता रखती है, बल्कि निर्यात को बढ़ावा देने और भारत की वैश्विक पहचान को और मजबूत करने का भी एक प्रभावशाली साधन है। हालाँकि सिनेमा अपनी चकाचौंध और प्रेरणा से लोगों को आकर्षित करता रहेगा, लेकिन इसके आगे एक विशाल, जीवंत और बहुआयामी रचनात्मक अर्थव्यवस्था मौजूद है, जिसका पूर्ण दोहन अभी बाकी है। यदि भारत अपनी प्राचीन सभ्यता की विरासत को समकालीन नवाचार और वैश्विक सोच के साथ जोड़ने में सफल होता है, तो ऑरेंज इकॉनमी आने वाले समय में उसकी सबसे प्रभावशाली सॉफ्ट पावर बनकर उभर सकती है।
| मुख्य प्रश्न: “सांस्कृतिक समावेशिता और सभ्यतागत निरंतरता एक लचीली रचनात्मक अर्थव्यवस्था को आकार देने में भारत की प्रमुख संपत्ति हैं।” ऑरेंज इकोनॉमी के साथ भारत की भागीदारी के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें। |