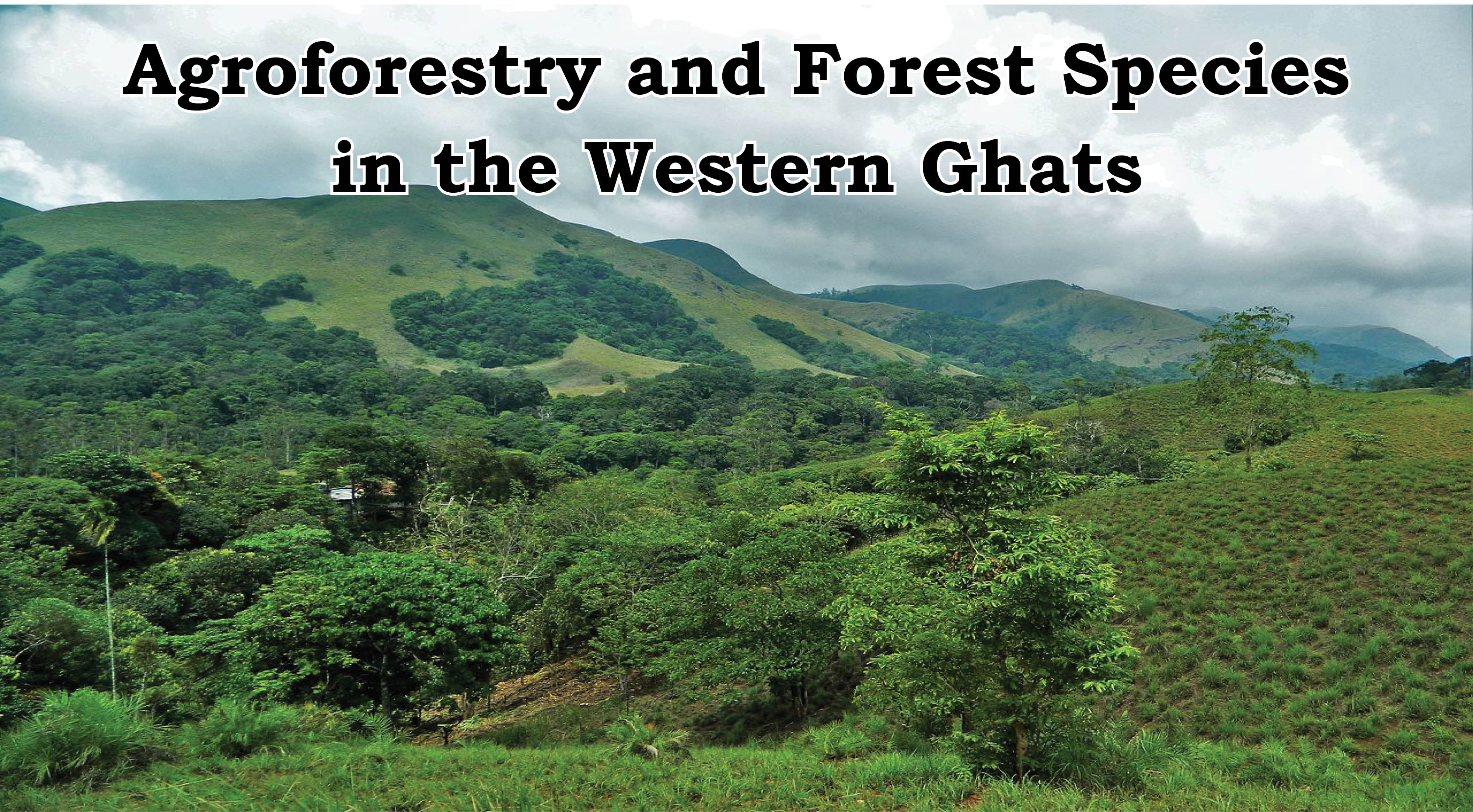परिचय
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र पश्चिमी घाट ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभावों का सामना कर रहा है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में यह पता चला है कि इस क्षेत्र की उष्णकटिबंधीय कृषि वानिकी और देशी वन प्रजातियाँ बढ़ते तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील होती जा रही हैं। यह अध्ययन विशेष रूप से भविष्य में संभावित जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 2023 में कर्नाटक के सिरसी के पास होसगड्डे गांव में 4.5 महीने की अवधि में किया गया, जिसमें पौधों की गर्मी से होने वाले तनाव के प्रति शारीरिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया गया और उनके तापीय सुरक्षा मार्जिन का मूल्यांकन किया गया।
अनुसंधान पद्धति और फोकस:
अध्ययन में T₅₀ नामक एक पैरामीटर का उपयोग किया गया, यह वह तापमान है जिस पर पत्तियों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता आधी रह जाती है। यह सीमा पौधों के अध्ययन में इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि किस तापमान के बाद कोशिकाओं को इतना नुकसान होता है कि वे ठीक नहीं हो पातीं, जिससे पौधे की मृत्यु भी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कई प्रजातियों ने इन महत्वपूर्ण सीमाओं को पार करते हुए पत्ती के तापमान का अनुभव किया, जिससे बढ़ती चरम जलवायु परिस्थितियों से निपटने की उनकी क्षमता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुईं।
अध्ययन में जिन कृषि वानिकी प्रजातियों को शामिल किया गया, उनमें इलायची, काजू, चीकू, दालचीनी, नींबू, लौंग, कोको, कॉफी, काली मिर्च, रामबुतान, सिज़ीगियम और वेनिला जैसे व्यावसायिक रूप से महत्त्वपूर्ण पौधे शामिल थे। इनमें से कई प्रजातियाँ अत्यधिक गर्मी की छोटी अवधि से प्रभावित पाई गईं, जो लंबे समय में नुकसान पहुँचा सकती है, हालांकि ऐसे खतरनाक तापमान का सामना करने की अवधि अक्सर 10 मिनट से कम ही थी।
मुख्य निष्कर्ष
ताप तनाव और पत्ती तापमान प्रतिक्रिया
- तेज़ धूप के समय पत्तियों का तापमान अक्सर हवा के तापमान से 10–12 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है तथा कभी-कभी आस-पास की हवा का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है।
- कई पौधों की पत्तियों का तापमान उनके T₅₀ स्तर से ऊपर दर्ज किया गया, हालाँकि यह स्थिति आमतौर पर 10 मिनट से कम समय के लिए रही।
- ऐसी थोड़ी देर की गर्मी से हमेशा स्थायी नुकसान नहीं होता, लेकिन बार-बार गर्मी पड़ने पर और अगर साथ में पानी की कमी या रोग भी हो, तो नुकसान का खतरा बढ़ जाता है।
प्रजाति भेद्यता
- कोको, दालचीनी, कॉफी, नींबू और रामबुतान जैसे पौधे गर्मी के तनाव के प्रति ज़्यादा संवेदनशील पाए गए।
- इनमें पत्तियों पर काले धब्बे जैसी चोटें देखी गईं, जो इस बात का संकेत हैं कि गर्मी का दीर्घकालिक असर हो सकता है।
देशी प्रजातियों का अवलोकन
- देशी पेड़ों में, किंडल (एक पतझड़ी पेड़) ने बहुत ज़्यादा लेकिन अस्थिर गर्मी का सामना किया।
- आयरनवुड में हल्के तनाव के लक्षण दिखे, जो यह दर्शाता है कि वह ज़्यादातर कृषि वानिकी प्रजातियों की तुलना में ज़्यादा सहनशील है।
थर्मल सुरक्षा मार्जिन:
थर्मल सुरक्षा मार्जिन “यानी पत्तियों के तापमान और उनके T₅₀ सीमा के बीच का अंतर” अब घट रहा है। यह छोटा अंतर दर्शाता है कि पौधे विशेष रूप से कृषि वानिकी प्रजातियाँ पहले से ही अपनी सहनशीलता की सीमा के पास काम कर रही हैं और ज़्यादा संवेदनशील हो गई हैं।
भारत में कृषि वानिकी और कार्बन पृथक्करण
कृषि वानिकी, एक सतत भूमि उपयोग प्रणाली है जिसमें पेड़ों को फसलों के साथ मिलाकर उगाया जाता है, जिससे आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक स्तर पर कई तरह के लाभ मिलते हैं। भारत में यह तरीका लगभग 28.4 मिलियन हेक्टेयर में अपनाया गया है, जो देश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 8.65% है। खास बात यह है कि कृषि वानिकी भारत के कुल कार्बन भंडार में करीब 19.3% का योगदान देती है। यदि इसके लिए सही नीतियाँ और वित्तीय मदद मिलें, तो विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रणाली 2030 तक 2.5 बिलियन टन से अधिक CO₂-समतुल्य कार्बन को संग्रहित कर सकती है।
एआरआर और कार्बन वित्त
कृषि वानिकी, वनरोपण, पुनर्वनरोपण और पुनर्वनीकरण (एआरआर) पहलों के साथ निकटता से जुड़ी हुई है, जो भूमि पुनरुद्धार, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- हालाँकि, भारत की अत्यधिक खंडित भूमि स्वामित्व पद्धति वैश्विक कार्बन वित्त तक पहुँचने में एक महत्वपूर्ण बाधा प्रस्तुत करती है।
- लगभग 86.1% किसान छोटे या सीमांत हैं और दो हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती करते हैं, इसलिए उनकी बिखरी हुई प्रथाओं को अक्सर वैश्विक मानकों जैसे कि वेरा के सत्यापित कार्बन मानक (वीसीएस) और गोल्ड स्टैंडर्ड के तहत "सामान्य" माना जाता है।
- यह वर्गीकरण कई भारतीय किसानों को कार्बन क्रेडिट योजनाओं में भाग लेने से अयोग्य बनाता है, भले ही उनके प्रयासों का पर्यावरणीय मूल्य स्पष्ट हो।
कार्बन वित्त तंत्र में सुधार की आवश्यकता:
एक बड़ी चुनौती है “सामान्य अभ्यास” मानदंड का इस्तेमाल, जिसमें भारतीय कृषि वानिकी अक्सर इसकी प्रभावशीलता की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसकी पारंपरिक और व्यापक मौजूदगी की के कारण असफल हो जाती है। इसके अलावा, मौजूदा कार्बन वित्त मॉडल ज़्यादातर अमेरिका या ब्राज़ील जैसे देशों की बड़ी और एक जैसी कृषि व्यवस्था पर आधारित हैं, जो भारत की छोटी जोतों वाली खेती के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
यह ढाँचागत अंतर उस समय और जटिल हो जाता है जब किसानों में कृषि वानिकी के फायदों को लेकर जागरूकता की कमी हो, साथ ही पौधे लगाने, बाड़ लगाने और देखभाल की शुरुआती लागत भी ज़्यादा हो। ये सारी बातें इस प्रणाली को अपनाने में बाधा बनती हैं, खासकर उन ग्रामीण समुदायों में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं।
इन समस्याओं से निपटने के लिए कार्बन वित्त तंत्र में बदलाव ज़रूरी है। भारत की कृषि व्यवस्था की खास बातों को ध्यान में रखते हुए “अतिरिक्तता” की परिभाषा भारत के लिए अलग से तय की जानी चाहिए। नई नीतियों का मकसद ऐसे समावेशी मानक बनाना होना चाहिए, जो छोटे और सीमांत किसानों को भी कार्बन बाज़ार से जोड़ सकें।
इससे निवेश का बोझ घट सकता है, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ज़रिए किसानों को वृक्ष-फसल की अनुकूलता, सतत जल उपयोग और लंबी अवधि के भूमि प्रबंधन जैसे ज़रूरी विषयों को समझने में मदद मिलेगी।
कृषि वानिकी एकीकरण के लाभ:
- कृषि वानिकी को कार्बन वित्त से जोड़ने में बड़ी संभावनाएँ हैं। आर्थिक रूप से यह किसानों को कार्बन क्रेडिट और वृक्ष आधारित उत्पादों के ज़रिए आय के नए स्रोत दे सकता है।
- पर्यावरण के लिहाज़ से, कृषि वानिकी मिट्टी की उर्वरता को बेहतर बनाती है, पानी को ज़मीन में रोकने की क्षमता बढ़ाती है और बंजर ज़मीन को फिर से उपजाऊ बनाने में मदद करती है।
- सामाजिक स्तर पर, इस प्रणाली से मिलने वाली अतिरिक्त आमदनी ग्रामीण आजीविका को मजबूत बना सकती है, मानसून की अनिश्चितता पर निर्भरता को घटा सकती है और अंततः खेती करने वाले समुदायों को ज़्यादा सक्षम और सुरक्षित बना सकती है।
निष्कर्ष और आगे की राह:
पश्चिमी घाट अध्ययन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कृषि वानिकी फसलों और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण देशी वन प्रजातियों दोनों के लिए गर्मी के तनाव के जोखिम का आकलन करने और उसे कम करने की तत्काल आवश्यकता का संकेत देता है। इसके साथ ही, भारत को अपने अद्वितीय कृषि परिदृश्य को समायोजित करने के लिए अपने कार्बन वित्त वास्तुकला को फिर से परिभाषित करना चाहिए।
भविष्य की जलवायु परिस्थितियों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए:
- ताप-सहिष्णु प्रजातियों और किस्मों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- रोपण कार्यक्रम और छत्र प्रबंधन तकनीकें गर्मी के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं।
- कृषि वानिकी की पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए संस्थागत समर्थन, नवीन नीतिगत ढांचे और समावेशी कार्बन वित्त तंत्र महत्वपूर्ण हैं।
भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां वह जलवायु विज्ञान, नीति सुधारों और ग्रामीण सशक्तिकरण को एकीकृत करके टिकाऊ कृषि वानिकी में वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व कर सकता है।
| मुख्य प्रश्न: कृषि वानिकी जलवायु-लचीली रणनीति के रूप में उभरी है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। पश्चिमी घाटों के हाल के अध्ययनों के प्रकाश में, कार्बन पृथक्करण और जलवायु अनुकूलन में कृषि वानिकी की भूमिका की जांच करें। कार्बन वित्त तक न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है? |